सभ्यता के अदृश्य निर्माता भारतीय शिल्पकार: विश्वकर्मा जयंती विशेष
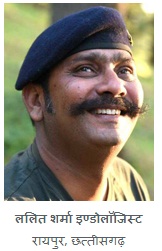 मानव सभ्यता के विकास का जहाँ भी वर्णन होता है वहां स्वत: ही तकनीकि रुप से दक्ष परम्परागत शिल्पकारों के काम का उल्लेख होता है। क्योंकि परम्परागत शिल्पकार के बिना मानव सभ्यता, संस्कृति तथा विकास की बातें एक कल्पना ही लगती हैं। शिल्पकारों ने प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक विभिन्न स्वरुपों में (लोहकार, रथकार, सोनार, ताम्रकार, शिल्पकार-वास्तुविद) अपने कौशल से शस्य श्यामला धरती को सजाने में कोई भी कसर बाकी नहीं रखी।
मानव सभ्यता के विकास का जहाँ भी वर्णन होता है वहां स्वत: ही तकनीकि रुप से दक्ष परम्परागत शिल्पकारों के काम का उल्लेख होता है। क्योंकि परम्परागत शिल्पकार के बिना मानव सभ्यता, संस्कृति तथा विकास की बातें एक कल्पना ही लगती हैं। शिल्पकारों ने प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक विभिन्न स्वरुपों में (लोहकार, रथकार, सोनार, ताम्रकार, शिल्पकार-वास्तुविद) अपने कौशल से शस्य श्यामला धरती को सजाने में कोई भी कसर बाकी नहीं रखी।
समस्त ऐषणाओं से परे एक साधक की तरह परम्परागत शिल्पकार अपने औजारों के प्रयोग से मानव जीवन को सरल-सहज एवं सुंदर बनाने का उद्यम कर रहे हैं। आज समस्त सृष्टि जिस सुवर्ण रुप में दृष्टिगोचर हो रही है वह हमारे परम्परागत शिल्पकारों के खून पसीने एवं श्रम की ही देन है। इससे हम इंकार नहीं कर सकते। यह बात हम गर्व से कह सकते हैं।
भारत में शिल्पकार्य का लाखों साल पुराना इतिहास है। आज जिसे हम इंड्रस्ट्रीज कहते हैं उसे वैदिक काल मे शिल्पशा्स्त्र या कला ज्ञान कहते थे। इसी ज्ञान विज्ञान के अधिष्ठाता भगवान विश्वकर्मा की जयंती माध सुदी त्रयोदशी को भारत में धूमधाम से मनाई जाती है।
महर्षि दयानंद कहते हैं – विश्वं सर्वकर्म क्रियामाणस्य स: विश्वकर्मा सम्यक सृष्टि का सृजन कर्म जिसकी क्रिया है, वह विश्वकर्मा है। भारत में ज्ञान विज्ञान के जानने वाले विश्वकर्मा या शिल्पी कहलाते थे। उस समय हमारा विज्ञान चरम सीमा पर था। ग्रहों की चाल जानने के लिए वेध चक्र और तुरीय यन्त्र (दूरबीन) बनाया गया, इसी तरह इनके पास कम्पास भी था। कम्पास का सिद्धांत चुम्बक की सुई पर अवलंबित है।
वैशेषिक दर्शन में कणाद मुनि लिखते हैं कि–
“मणिगमनं सू्च्यभिसर्पणमदृष्टकारणम् । “
अर्थात चुमबक की सुई की ओर लोहे के दौड़ने का कारण अदृष्ट है, यह लोह चुम्बक सुई के अस्तित्व का प्राचीनतम प्रमाण है।
इस तरह हस्तलिखित शिल्प संहिता, जो गुजरात के अणहिलपुर के जैन पुस्तकालय मे है, उसमे ध्रुवमत्स्य यंत्र बनाने की विधि स्पष्ट रुप से लिखी मिलती है। इसके साथ ही इस शिल्प संहिता में थर्मा मीटर और बैरो मीटर बनने की भी विधि लिखी है। वहां लिखा है कि-
” पारदाम्बुजसूत्राणि शुक्लतैलजलानि च। बीजानि पांसवस्तेषु।”
अर्थात पारा, सूत, तेल और जाल के योग से यह यन्त्र बनता है। शिल्प संहिताकार कहते हैं कि इस यन्त्र के निर्माण से ग्रीष्म आदि ऋतुओं का ज्ञान होता था तथा जाना जाता था कि कितनी सर्दी और गर्मी है। इनका वर्णन सिद्धांत शिरोमणि में भी है। इसके अतिरिक्त वैदिक काल में धूप घडी, जल घडी और बालुका घडी का भी निर्माण कर लिया गया था।
ज्योतिष ग्रंथों में लिखा है कि-
तोययंत्रकपालाद्यैर्मयुरनरवानरै:। ससूत्ररेणुगर्भश्च सम्यक्कालंअ प्रसाधयेत्।
जल यंत्र से समय जाना जाता है, मयूर,नर,वानर की आकृति के यन्त्र बनाकर उनमे बालू भरने और एक ओर का रेणु सूत्र दुसरे में गिरने से भी समय नापने का यन्त्र बन जाता है। इस प्रकार के दूरबीन, कम्पास, बैरोमीटर, और घडी आदि यंत्रों के बन जाने से प्राचीन काल में ग्रहों की चाल, उनसे उत्पन्न हुए वायु वेग की दिशा, गर्मी का पारा और समय आदि का ज्ञान संपादन करने में सुविधा होती थी।
इतना ही नहीं, किन्तु उन्होंने स्वयंवह नामक यन्त्र भी बना लिया था। जो गर्मी या सर्दी पाकर अपने आप चलने लगता था। इसका वर्णन सिद्धांत शिरोमणि में इस प्रकार आया है-
तुंगबीजसमायुक्तं गोलयंत्र प्रसाधयेत्। गोप्यमेतत् प्रकाशोक्तं सर्वगम्यं भवेदिह।
अर्थात पारा भरकर इस गोल यन्त्र को बनावें। यह यंत्र थोड़ी सी भी हवा चलने से, गर्मी पाकर अपने आप ही चल पड़ता है था। तूफान और मानसून जानने के लिए आज तक जितने भी यंत्र बने हैं, इसकी खूबी को एक भी नहीं पकड़ पाया है।
भारत वैदिक काल में वैज्ञानिक प्रगति के उत्कर्ष पर था। जिसे इस स्थिति में पहुँचाने के लिए विश्वकर्माओं ने अपनी सम्पूर्ण कार्य कुशलता का परिचय दिया तथा समाज को भौतिकता युक्त शिष्ट एवं सभ्य बनने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।




