रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे : रेल दिवस विशेष

भारत रुपी शरीर की धमनियाँ मैं रेलगाड़ी को ही मानता हूँ, जिस तरह शरीर में रक्त प्रवाह बनाए रखने में धमनियों का योगदान होता है उसी तरह भारत को चलाने के लिए रेलगाड़ियों का मुख्य भूमिका है। वर्तमान काल में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, जिसने रेलगाड़ी देखी न होगी या उसकी सवारी न की होगी। भारत में रेलगाड़ी के संचालन का अपना एक समृद्ध इतिहास है। प्रत्येक व्यक्ति के साथ रेलायात्रा का कोई न कोई संस्मरण जुड़ा हुआ है, कोई भी इससे अछूता नहीं है। कम खर्च में यात्रा कराने वाला यह साधन घुमक्कड़ों की पहली पसंद रहा है। इसके साथ नानी दादी की भी कहानियों के साथ राजे रजवाड़ों की ठसक भी जुड़ी हुई है। भारतीय लोकगीतों का विषय भी रेल बनी, कभी बिरहा के गीत गाये गये तो कभी आने की खुशी के, कभी साजन के जाने का दुख तो कभी साजन के आने की खुशी। इस तरह रेल आम आदमी के सुख दुख की हमेशा से साथी रही है।
भारतीय उपमहाद्वीप में रेल परिवहन का इतिहास न केवल ब्रिटिश शासन से जुड़ा हुआ है, बल्कि यह देशी रियासतों के आधुनिकता की ओर बढ़ते कदमों का भी परिचायक रहा है। भारत में रेलगाड़ियों की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को मानी जाती है, जब पहली यात्री ट्रेन बोरीबंदर (वर्तमान मुंबई) से ठाणे तक चली। यह कुल 34 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली भाप इंजन से संचालित ट्रेन थी, जिसमें 400 से अधिक यात्री सवार थे। इस ऐतिहासिक यात्रा ने एक नए युग का आरंभ किया, जिसने भारत के भूगोल, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना को बदल दिया।
रेलवे की शुरुआत और विस्तार का प्राथमिक उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के लिए प्रशासनिक नियंत्रण को आसान बनाना, सेना की तेज़ आवाजाही सुनिश्चित करना और देश के कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुँचाकर उसे ब्रिटेन भेजना था। इसलिए प्रारंभिक रेलवे परियोजनाएँ मुख्य रूप से बंदरगाहों से देश के भीतरी हिस्सों तक बनाईं गईं। इन परियोजनाओं को “गारंटीड रिटर्न” योजना के अंतर्गत निजी अंग्रेज़ी कंपनियों को सौंपा गया। ईस्ट इंडियन रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, मद्रास रेलवे, बंगाल नागपुर रेलवे जैसी कंपनियाँ इस समय सक्रिय रहीं।
हालाँकि रेलवे का मूल प्रबंधन और रणनीतिक दिशा ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में था, परंतु भारत के देशी रजवाड़े यानी रियासतें भी इस विकास से अछूती नहीं रहीं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर स्वतंत्रता तक कई समृद्ध और शक्तिशाली रियासतों ने अपने-अपने क्षेत्रों में रेलवे लाइनों का निर्माण करवाया और स्वतंत्र रूप से रेलगाड़ियों का संचालन भी किया। यह न केवल उनके प्रशासनिक विकास का प्रतीक था, बल्कि उनकी तकनीकी समझ और आधुनिक सोच को भी दर्शाती है।
भारत के रजवाड़ों के पास अपनी-अपनी राजसी ट्रेनें होती थीं। ये ट्रेनें केवल परिवहन का साधन नहीं, बल्कि चलता-फिरता महल होती थीं। इन रेलों के डिब्बे पूरी तरह लकड़ी के होते थे, जिनमें सोने-चांदी की कारीगरी, रेशमी पर्दे, कीमती फर्नीचर, राजसी बिस्तर और संगमरमर के बाथरूम होते थे। कुछ रियासतों ने तो बाथटब तक फिट करवा रखे थे। महाराजाओं के स्वाद का ख्याल रखने के लिए ट्रेन में चलती रसोई होती थी, जहाँ शाही बावर्ची ताज़ा खाना पकाते थे। कई बार अलग-अलग व्यंजनों के लिए अलग रसोइए और स्टाफ तैनात रहते थे।
महाराजाओं के साथ उनके अंगरक्षक, दरबारी, सेवक, शाही नौकर, राज वैद्य, पुरोहित, और खजांची तक ट्रेनों में साथ चलते थे। बड़ी रियासतों के लिए तो पूरी ट्रेन ही रिज़र्व रहती थी – जिसमें 6 से 10 डिब्बे तक सिर्फ राजा के इस्तेमाल में होते। जब कोई राजा यात्रा करता था, तो संबंधित रेलवे ज़ोन को पूर्व सूचना दी जाती थी और उस यात्रा को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती थी। स्टेशन पर कालीन बिछाए जाते थे, और गार्ड रेल पर ‘राजकीय यात्रा’ का चिन्ह लगाया जाता था। तत्कालीन समय के रजवाड़ों की गायकवाड़ एक्सप्रेस – बड़ौदा रियासत की ट्रेन, निज़ाम की विशेष गाड़ी – हैदराबाद के निज़ाम की स्वर्ण जड़ी सैलून ट्रेन, जोधपुर-बीकानेर राज ट्रेन – मरुस्थली क्षेत्र के राजपूतों की ट्रेन, पटियाला स्टेट मोती महल ट्रेन – महाराजा भूपिंदर सिंह द्वारा प्रायोजित आदि प्रसिद्ध थी
हैदराबाद रियासत द्वारा स्थापित निज़ाम्स गारंटीड स्टेट रेलवे इस दिशा में सबसे प्रमुख उदाहरण है। इस रेल प्रणाली की शुरुआत 1883 में हुई थी और यह वाडी से सिकंदराबाद, विजयवाड़ा तथा औरंगाबाद जैसे शहरों को जोड़ती थी। इस रेलवे का पूरा वित्तपोषण निज़ाम ने स्वयं किया था और इसका संचालन भी स्वतंत्र रूप से होता था। यह ब्रिटिश नेटवर्क से जुड़ी थी, लेकिन अपनी आंतरिक संरचना में यह पूर्णतः रियासती नियंत्रण में थी।
मध्य भारत की ग्वालियर रियासत ने 1895 में ग्वालियर लाइट रेलवे की स्थापना की, जो नैरो गेज पर आधारित थी और ग्वालियर से श्योपुरकलां तक फैली थी। यह रेलवे अपनी संकरी पटरी और लंबी दूरी के लिए प्रसिद्ध थी और कई दशकों तक दुनिया की सबसे लंबी नैरो गेज रेलवे मानी जाती रही। सिंधिया वंश द्वारा संचालित यह प्रणाली मुख्य रूप से प्रशासनिक सुविधा और स्थानीय व्यापार को सुगम बनाने के लिए विकसित की गई थी।
बड़ौदा रियासत, जिसे आज का गुजरात क्षेत्र माना जाता है, गायकवाड़ वंश के अधीन थी और वहाँ भी रेलवे का विकास हुआ। बड़ौदा स्टेट रेलवे ने अहमदाबाद, सूरत और अन्य प्रमुख शहरों को जोड़ा। यह नेटवर्क बाद में बॉम्बे, बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे (BB&CI) में सम्मिलित हो गया।
राजस्थान की जोधपुर और बीकानेर रियासतों ने मिलकर जोधपुर-बिकानेर रेलवे का निर्माण किया, जो 1889 में अस्तित्व में आई। यह एक संयुक्त उपक्रम था जो जोधपुर, बीकानेर और बठिंडा जैसे क्षेत्रों को जोड़ता था। 1924 में यह रेलवे दो भागों में विभाजित हो गई, लेकिन उस समय तक यह क्षेत्रीय और सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण बन चुकी थी।
इसी प्रकार सौराष्ट्र क्षेत्र की कई छोटी-छोटी रियासतों, जैसे जूनागढ़, भावनगर, राजकोट, जामनगर आदि ने मिलकर काठियावाड़ राज्य रेलवे नामक नेटवर्क का विकास किया। इन रेल परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य स्थानीय व्यापार को प्रोत्साहन देना और प्रशासनिक सम्पर्क बढ़ाना था। रेलवे संचालन की दृष्टि से इन रियासतों ने स्थानीय स्तर पर इंजीनियरों, गार्डों, स्टेशन मास्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की। कुछ रियासतों ने ब्रिटिश इंजीनियरों की मदद भी ली, विशेषकर तकनीकी मामलों में। सुरक्षा और संचालन व्यवस्था पूरी तरह रियासती सेना या नियुक्त कर्मचारियों के जिम्मे होती थी। वहीं कुछ रियासतों में केवल राजपरिवार और उनके मेहमानों के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन भी होता था, जो विलासिता और भव्यता का प्रतीक थीं।
यह भी स्मरणीय है कि उस समय भारत एक संपूर्ण उपमहाद्वीप था, जिसमें आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश भी सम्मिलित थे। ब्रिटिश काल में रेलवे नेटवर्क इस सम्पूर्ण क्षेत्र को जोड़ता था। यात्री बिना किसी सीमा के कलकत्ता (अब कोलकाता) से कराची या पेशावर तक यात्रा कर सकते थे। दिल्ली से लाहौर, लखनऊ से पेशावर, मुंबई से कराची, कोलकाता से ढाका और चटगाँव तक ट्रेनें नियमित रूप से चलती थीं। दिल्ली–लाहौर, जोधपुर–कराची, और सियालदह–ढाका जैसे मार्ग विशेष रूप से व्यस्त और महत्वपूर्ण माने जाते थे। उस समय इन मार्गों पर पंजाब मेल, ढाका मेल, और फ़्रंटियर मेलl जैसी प्रसिद्ध ट्रेनें चला करती थीं। ये ट्रेनें केवल लोगों को नहीं, बल्कि संस्कृतियों, व्यवसायों और रिश्तों को भी जोड़ा करती थीं।
स्वतंत्रता के बाद, जब देश का विभाजन हुआ, तब ये रेल मार्ग राजनीतिक सीमाओं में बँट गए। कई मार्ग बंद कर दिए गए, कुछ सीमित सेवाओं के रूप में जारी रहे। लेकिन इससे पहले, भारतीय रेलवे एक अखंड व्यवस्था थी जो उपमहाद्वीप की नाड़ियों में रक्त की तरह बहती थी। 1951 तक लगभग सभी देशी रियासतों की रेल प्रणालियाँ भारतीय रेल में विलीन हो चुकी थीं और एक संगठित, केंद्रीकृत रेल प्रबंधन की नींव रखी गई। इस तरह भारतीय रेलवे, जो कभी औपनिवेशिक उद्देश्यों के तहत शुरू हुई थी, स्वतंत्र भारत में जन-जन की जीवनरेखा बन गई।
कभी मुंबई और थाणे के बीच 34 किलोमीटर चली ट्रेन का आज भारत में 2025 तक नेटवर्क लगभग 135,207 किलोमीटर (ट्रैक लंबाई) है, जिसमें रूट लंबाई लगभग 69,181 किलोमीटर है। यह नेटवर्क 7,325 से अधिक रेलवे स्टेशनों को कवर करता है। 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय रेलवे प्रतिदिन औसतन 2.4 करोड़ (24 मिलियन) यात्रियों को ढोता है। हालांकि, त्योहारी सीजन (जैसे छठ पूजा 2024) में यह संख्या बढ़कर 3 करोड़ तक पहुंच सकती है। 2023-24 में भारतीय रेलवे ने औसतन 11,724 मालगाड़ियां संचालित कीं, जो प्रतिदिन लगभग 43.5 लाख टन (4.35 मिलियन टन) माल ढोती हैं।
इस तरह हम देखते हैं कि भारतीय रेल न सिर्फ़ सवारी या माल ढोने का काम करती है बल्कि संस्कृतियों एवं व्यावसायिक रिश्तों को भी जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। वर्तमान में वंदे भारत जैसे ट्रेने भारत का गौरव बढा रही है एवं भविष्य में बुलेट ट्रेन पर भी कार्य हो रहा है। इस तरह भारतीय रेल का इतिहास समृद्ध रहा है और भविष्य भी उज्जवल होगा।




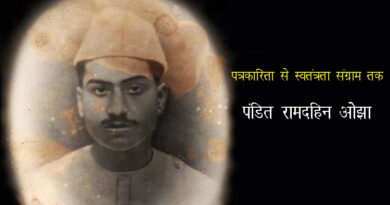
बहुत ही सुंदर आलेख और जानकारियां
बहुत सुंदर जानकारी भईया👌👌👌