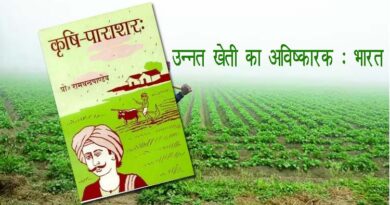छत्तीसगढ़ में दशहरा मनाने की अद्भूत परम्परा

दशहरा भारत का एक प्रमुख लोकप्रिय त्योहार है। इसे देश के कोने कोने में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। वास्तव में यह त्योहार असत्य के उपर सत्य का और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। श्रीराम सत्य के प्रतीक हैं। रावण असत्य के प्रतीक हैं। विजय प्राप्त करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है और हमें शक्ति मां भवानी की पूजा-अर्चना से मिलती है। इसके लिए अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमीं तक मां दुर्गा की पूजा-अर्चना करते हैं और दसमीं को दस सिर वाले रावण के उपर विजय प्राप्त करते हैं। कदाचित् इसी कारण दशहरा को ‘‘विजयादशमी‘‘ कहा जाता है।
वास्तव में रावण अजेय योद्धा के साथ साथ प्रकांड विद्वान भी थे। उन्होंने अपने बाहुबल से देवताओं, किन्नरों, किरातों और ब्रह्मांड के समस्त राजाओं को जीतकर अपना दास बना लिया था। मगर वे अपनी इंद्रियों कों नहीं जीत सके तभी तो वे काम, क्रोध, मद और लोभ के वशीभूत होकर कार्य करते थे। यही उन्हें असत्य के मार्ग में चलने को मजबूर करते थे। इसी के वशीभूत होकर उन्होंने माता सीता का हरण किया और श्रीराम के हाथों मारे गये। श्रीराम की विजय की खुशी में ही लोग इस दिन को ‘‘दशहरा‘‘ कहने लगे और प्रतिवर्ष रावण के प्रतिरूप को मारकर दशहरा मनाने लगे।
यहां यह बात विचारणीय है कि आज हम गांव गांव और शहर में इस दिन रावण की आदमकद प्रतिमा बनाकर जलाकर दशहरा मनाते हैं। इस दिन रावण की प्रतिमा को जलाकर घर लौटने पर मां अपने पति, बेटे और नाती-पोतों तथा रिश्तेदारों की आरती उतारकर दही और चांवल का तिलक लगाती है और मिष्ठान खाने के लिए पैसे देती है। कई घरों में नारियल देकर पान-सुपारी खिलाने का रिवाज है। इस दिन अपने मित्रों, बड़े बुजुर्गों, छोटे भाई-बहनों, माताओं आदि सबको ‘‘सोनपत्ति‘‘ देकर यथास्थिति आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। लोग अपने मित्रों से गले मिलकर रावण मारने की बधाई देते हैं।
कहीं कहीं दशहरा के पहले ‘रामलीला‘ का मंचन होता है और रामराज्य की कल्पना की जाती है। रायगढ़ में मथुरा की नाटक मंडली आकर रामलीला का मंचन करती थी। छत्तीसगढ़ में रामलीला के लिए अकलतरा और कोसा बहुत प्रसिद्ध था। इसी प्रकार रासलीला के लिए नरियरा और नाटक के लिए शिवरीनारायण बहुत प्रसिद्ध था। टी.बी. की चकाचैंध ने रामलीला, रासलीला और नाटकों के मंचन को प्रभावित ही नहीं किया बल्कि समाप्त ही कर दिया है। यह एक विचारणीय प्रश्न है।
दशहरा के पूर्व शक्ति की साधना की जाती है। विभिन्न स्थानों में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है। आज दुर्गा की झांकियों के लिए बिलासपुर का नाम कलकत्ता के बाद आने लगा है। नवरात्रि में पूरा बिलासपुर दुर्गामय हो जाता है। राजे-रजवाड़े के समय मां दुर्गा की प्रतिमा स्ािापित नहीं किये जाते थे बल्कि देवी मंदिरों में जंवारा बोया जाता था और विशेष पूजा-अर्चना की जाती थी। देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि दी जाती थी। छत्तीसगढ़ के प्रायः सभी रियासतों और जमींदारी में कोई न कोई देवी प्रतिष्ठित हैं जो उनकी ‘कुलदेवी‘ हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि देवियों की पूजा से राजा जहां शक्ति संपन्न होता था वहीं रियाया की सुरक्षा के शक्ति संचय आवश्यक भी था। वे अपनी मान्यता के अनुसार देवी के नाम पर अपनी राजधानी का नामकरण किये हैं। चंद्रपुर की चंद्रसेनी देवी, दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी देवी, सारंगढ़ की सारंगढ़हीन देवी और संबलपुर की समलेश्वरी देवी आदि।
छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से महामाया और समलेश्वरी देवी प्रतिष्ठित हैं। वास्तव में ये दोनों देवी दो प्रमुख रियासत क्रमशः रत्नपुर और संबलपुर की कुलदेवी हैं। छत्तीसगढ़ की रियासतें और जमींदारी या तो रत्नपुर से जुड़ी थी या फिर संबलपुर रियासत से। यहां के सामंत मित्रतावश वहां की देवियों को अपनी राजधानी में स्थापित करके उन्हें अपनी कुलदेवी मान लिए। इसके अलावा यहां अनेक देवियां क्षेत्रीयता का बोध कराती हैं, जैसे- सरगुजा की सरगुजहीन दाई, चंद्रपुर की चंद्रसेनी देवी, डोंगरगढ़ की बमलेश्वरी देवी, अड़भार की अष्टभुजी देवी, कोरबा की सर्वमंगला देवी, दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी देवी, जशपुर की कालीमाई आदि। इन देवियों की प्राण प्रतिष्ठा कई रियासतों और जमींदारी के निर्माण की गाथा से जुड़ी हैं। यहां नवरात्रि में देवियों की विशेष पूजा-अर्चना और दशहरा मनाने की विशिष्ट परंपरा रही है जो आज काल कवलित होती जा रही है। कहीं कहीं इसके अवशेष अवश्य देखे जा सकते हैं।
सक्ती राज परिवार में आज भी होती है लकड़ी के तलवार की पूजा:-
इतिहास के पन्नों को उलटने से पता चलता है कि सक्ती रियासत यहां के शासक के शौर्य के प्रदर्शन के फलस्वरूप निर्मित हुआ था। पूर्व में यह क्षेत्र संबलपुरराज के अंतर्गत था। यहां के शासक संबलपुर रियासत की सेना में महत्वपूर्ण ओहदेदार थे और अपनी शूर वीरता के लिए बहुत चर्चित थे। यह दो जुड़वा भाई हरि और गुजर की कहानी है जो लकड़ी के तलवार को अपना हथियार बनाये थे। उसी तलवार से शिकार भी करते थे। जब संबलपुर के राजा कल्याणसाय को पता चला कि उनकी विशाल सेना में दो अधिकारी ऐसे हैं जो लकड़ी की तलवार से लड़ते हैं। तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ था। वे विचार करने लगे कि कहीं हमारी सेना का यह तौहीन तो नहीं है ? उन्होंने तत्काल आदेश दिया कि इस वर्ष विजयादशमी पर्व में मां समलेश्वरी में भैंस की बलि उन्हीं जुड़वा भाईयों की तलवार से दी जायेगी। शर्त यह होगी कि भैंस का सिर लकड़ी के तलवार के एक ही वार से कटना चाहिये अन्यथा दोनों भाईयों का सिर कलम कर दिया जायेगा…?
दशहरा के दिन संबलपुर में विशाल जन समुदाय के बीच राजा कल्याणसाय ने देखा कि हरि और गुजर ने अपने लकड़ी के तलवार से एक ही वार से भैंस की सिर काट डाला, अविश्वसनीय किंतु सत्य। विशाल जन समुदाय ने करतल ध्वनि से दोनों भाईयों का स्वागत किया। राजा उनके शौर्य से प्रसन्न होकर घोषणा की कि ‘तुम दोनों एक ऐसे क्षेत्र का विस्तार करो जो शक्ति का प्रतीक हो और जिसके तुम दोनों जमींदार होगे।‘ तब दोनों भाईयों ने एक ऐसा करतब दिखाया जो सबको पुनः आश्चर्य में डाल दिया। उन्होंने राजा बहादुर से निवेदन किया कि ‘हम दोनों सूर्योदय से सूर्यास्त तक पैदल जितनी भूमि नाप सकेंगे, हम उसी भूमि के अधिकारी होंगे।‘ उनकी बात राजा ने मान ली। शर्त के मुताबिक हरि और गुजर दिन भर में 138 वर्ग मील का क्षेत्र पैदल चलकर तय किया और शौर्य के प्रतीक ‘‘सक्ती रियासत‘‘ की स्थापना की। उनके शौर्य गाथा में एक जनश्रुति और प्रचलित है जिसके अनुसार दोनों भाई एक बार निहत्थे एक आदमखोर शेर से लड़े थे। रियासत बनने के बाद सक्ती जमींदारी में प्रजा बड़ी सुखी थी। आगे चलकर यहां के जमींदार रूपनारायण सिंह को अंग्रेजों ने सन् 1892 में ‘‘राजा बहादुर‘‘ का सनद प्रदान किया। आज भी यहां दशहरा पर्व में देवी की पूजा-अर्चना और लकड़ी के तलवार की पूजा की जाती है।
सारंगढ़ में गढ़ भेदन की परंपरा:-
वर्तमान सारंगढ़ पूर्व में सारंगपुर कहलाता था। सारंग का शाब्दिक अर्थ है-बांस। अर्थात् यहां प्राचीन काल में बांसों का विशाल जंगल था। कहा तो यहां तक जाता है कि यहां के सैनिकों के हथियार भी बांस के हुआ करते थे। यहां के राजा के पूर्वज बालाघाट जिलान्तर्गत लांजी से पहले फूलझर आये। यहां के जमींदार उनके रिश्तेदार थे। बाद में श्री नरेन्द्रसाय को संबलपुर के राजा ने सैन्य सेवा के बदले सारंगढ़ परगना पुरस्कार में दिया था। आगे चलकर वे सारंगढ़ के जमींदार बने थे। यहां के राजा कल्याणसाय (सन् 1736 से 1777) हुये, जिन्हें मराठा शासक ने ‘‘राजा‘‘ की पदवी प्रदान की थी। यहां के राजा संग्रामसिंह (सन् 1830 से 1872) को अंग्रेजों ने ‘‘फ्यूडेटरी चीफ‘‘ बनाया था।
यहां के राजा की कुलदेवी ‘‘सम्लाई देवी‘‘ है, जो गिरि विलास पैलेस परिसर में आज भी प्रतिष्ठित है। प्राप्त जानकारी के अनुसार समलेश्वरी देवी की स्थापना सन् 1692 में की गयी थी। सारंगढ़ छत्तीसगढ़ का उड़ीसा प्रांत से लगा सीमांत तहसील मुख्यालय है। यहां छत्तीसगढ़ी और उड़िया परंपरा आज भी देखने को मिलती है। यहां के प्रमुख त्योहारों में रथयात्रा और दशहरा है। रथयात्रा में जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी सवारी पूरे नगर में बड़े उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है वहीं दशहरा में गढ़ भेदन की परंपरा यहां के मुख्य आकर्षक हैं।
शिवरीनारायण रोड में नगर से 4 कि.मी. की दूरी पर खेलभाठा में गढ़ भेदन किया जाता है। यहां चिकनी मिट्ठी का प्रतीकात्मक गढ़ (मिट्ठी का ऊंचा टीला) बनाया जाता है और उसके चारों ओर पानी भरा होता है। गढ़ के सामने राजा, उसके सामंत और अतिथियों के बैठने के लिए स्टेज बनाया जाता था, जिसके अवशेष यहां आज भी मौजूद है। विभिन्न ग्रामों से दशहरा मनाने आये ग्रामीण जन इस गढ़ भेदन में प्रतियोगी होते थे। वे इस मिट्ठी के गढ़ में चढ़ने का प्रयास करते और फिसल कर पानी में गिर जाते हैं। पानी में भीगकर पुनः गढ़ में चढ़ने के प्रयास में गढ़ में फिसलन हो जाता था। बहुत प्रयत्न के बाद ही कोई गढ़ के शिखर में पहुंच पाता था और विजय स्वरूप गढ़ की ध्वज को लाकर राजा को सौंपता था। करतल ध्वनि के बीच राजा उस विजयी प्रतियोगी को तिलक लगाकर नारियल और धोती देकर सम्मानित करते थे।
फिर राजा की सवारी राजमहल में आकर दरबारेआम में बदल जाती थी जहां दशहरा मिलन होता था। ग्रामीणजन अपने राजा को इतने करीब से देखकर और उन्हें सोनपत्ती देकर, उनके चरण वंदन कर आल्हादित हो उठते थे। सहयोगी सामंत, जमींदार और गौटिया नजराना पेश कर अपने को धन्य मानते थे। अंत में मां समलेश्वरी देवी की पूजा अर्चना करके खुशी खुशी घर को लौटते थे। राजा नरेशचंद्र सिंह ने यहां के दशहरा उत्सव को अधिक आकर्षक बनाने के लिए मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्रियों को आमंत्रित किया करते थे जो गढ़ भेदन के समय स्टेज में राजा के बगल में बैठते थे। यहां के दशहरा उत्सव में भाग लेने वाले मुख्य मंत्रियों में डाॅ. कैलासनाथ काटजू, श्री भगवंतराव मंडलोई, श्री द्वारिकाप्रसाद मिश्र, राजा गोविंदनारायण सिंह और पंडित श्यामाचरण शुक्ल प्रमुख थे। यहां भी बांस के हथियारों की पूजा की जाती है।
चंद्रपुर में नवमीं को दशहरा:-
उड़ीसा के संबलपुर रियासत के अंतर्गत चंद्रपुर एक छोटी जमींदारी थी। जब मध्यप्रदेश बना तब चंद्रपुर को बिलासपुर जिलान्तर्गत जांजगीर तहसील में सम्मिलित किया गया था जो महानदी और मांड नदी के तट पर स्थित है। यहां की अधिष्ठात्री चंद्रसेनी देवी हैं। इस मंदिर की स्थापना के बारे में एक किंवदंति प्रचलित है। जिसके अनुसार चंद्रसेनी देवी, सरगुजा की सरगुजहीन दाई और संबलपुर की समलेश्वरी देवी की छोटी बहन है। समलेश्वरी देवी रायगढ़ और सारंगढ़ में भी विराजमान हैं। एक बार किसी बात को लेकर चंद्रसेनी देवी नाराज होकर सरगुजा को छोड़कर निकल जाती हैं। सरगुजा की सीमा को पार करके उदयपुर (वर्तमान धरमजयगढ़) होते हुए रायगढ़ आ जाती है। यहां समलेश्वरी देवी उन्हें रोकने का बहुत प्रयास करती है लेकिन चंद्रसेनी देवी यहां भी नहीं रूकती और दक्षिण दिशा में आगे बढ़ जाती है। रास्ते में वह सोचने लगती है कि अगर सारंगढ़ में समलेश्वरी दीदी पुनः रोकेगी तो मैं क्या करूंगी..? इस प्रकार सोचते हुए वह महानदी के तट में पहुंच गई और वहां विश्राम करने लगी। सफर की थकान से उन्हें गहरी नींद आ गई।
एक बार संबलपुर के राजा की सवारी महानदी पार करते समय और अनजाने में राजा के पैर की ठोकर मिट्ठी से दबी चंद्रसेनी देवी की लग गई जिससे उनकी निद्रा खुल गई। उन्होंने राजा को स्वप्न में निर्देश दिया कि तुमने मेरा अपमान किया है अगर तुमने महानदी के तट पर एक मंदिर निर्माण कराकर मेरी स्थापना नहीं करायी तो तुम्हारा सर्वनाश हो जायेगा..? तत्काल राजा ने मूर्ति को निकलवाकर महानदी के तट पर टीले के उपर एक मंदिर बनवाकर चंद्रसेनी देवी की स्थापना विधिवत करायी। आगे चलकर उनके नाम पर चंद्रपुर नगर बसा। आज चंद्रसेनी देवी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की अधिष्ठात्री देवी हैं। यहां प्रतिवर्ष बड़ी धूमधाम से नवरात्र पर्व में पूजा-अर्चना की जाती है। यहां ‘‘जेवरहा परिवार‘‘ को पूजा करने का अधिकार मिला है। अष्टमी के दिन यहां बलि देने की परंपरा है। यहां शुरू से ही भैंसा की बलि दी जाती है। और नवमी को विजय खुशी मनाते हुए विजयादशमीं (दशहरा) मनाया जाता है।
पूजा उत्सव सरगुजा रियासत का प्रमुख आकर्षण:-
सरगुजा रियासत में दशहरा उत्सव वास्तव में सरगुजहीन और महामाया देवी की पूजा-अर्चना का पर्व होता है। यहां दो देवियों-सरगुहीन (समलेश्वरी) और महामाया देवी की पूजा एक साथ होती है। इस प्रकार दो देवियों की पूजा एक साथ कहीं देखने को नहीं मिलता। शक्ति संचय का यह नवरात्र पर्व बड़ी श्रद्धा से यहां मनाया जाता है। अश्विन शुक्ल परवा के दिन महामाया देवी के मंदिर में कलश स्थापना का कार्य पूरा होता है। इसे ‘‘पहली पूजा‘‘ कहा जाता है। इसी दिन से सरगुजा रियासत के अंतर्गत आने वाले राजा, जमींदार, गौंटिया, किसान और ग्रामीण जन यहां इकठ्ठा होने लगते हैं। अष्टमी के दिन राजा की सवारी का विशाल जुलूस ‘‘बलि पूजा‘‘ के लिए नगर भ्रमण के बाद महामाया मंदिर पहुंचती थी। महामाया देवी को प्राचीन काल में नरबलि देने का उल्लेख तत्कालीन साहित्य में मिलता है। बाद में उसे बंद कर दिया गया और पशु बलि दी जाने लगी। इस दिन को ‘‘महामार‘‘ कहा जाता था। फिर दशहरा को राजा की सवारी पुनः देवी दर्शन कर नगर भ्रमण करती हुई राजमहल परिसर में पहुंचकर ‘‘मिलन समारोह‘‘ में परिवर्तित हो जाता था। उस समय राज परिवार के सभी सदस्य, अन्य सामंत, जमींदार, ओहदेदार विराजमान होते थे। ग्रामीणजन सोनपत्ती देकर उन्हें बधाई देते थे। उस दिन सरगुजा के लिए अविस्मरणीय होता था जिसका स्मरण कर आज भी वहां के लोग रोमांचित हो उठते हैं। सरगुजा में देवी पूजा का वर्णन सुप्रसिद्ध कवि पंडित शुकलाल पांडेय ने ‘‘छत्तीसगढ़ गौरव‘‘ में की है:-
लखना हो शक्ति उपासना तो चले सिरगुजा जाईये।।
रत्नपुर जहां नरबलि दी जाती थी:-
रत्नपुर कलपुरी राजाओं की वैभवशाली राजधानी थी। यह नगर महामाया देवी की उपस्थिति के कारण ‘‘शक्तिपीठ‘‘ कहलाता है। रत्नपुर का राजधानी के रूप में निर्माण महामाया देवी के आदेश-आशीष का ही प्रतिफल है। तत्कालीन साहित्य में उपलब्ध जानकारी के अनुसार रत्नपुर में महामाया देवी की मूर्ति को मराठा सैनिकों ने बंगाल अभियान से लौटते समय सरगुजा से लाकर प्रतिष्ठित किया था। राजा की सरगुजा में महामाया देवी की पूर्ति बहुत अच्छी लगी और वे उन्हें अपने साथ नागपुर ले जाना चाहते थे। इसी उद्देश्य से वे उस मूर्ति को वहां से उठाना चाहे लेकिन मूर्ति टस से मस नहीं हुई। हारकर राजा देवी के सिर को ही काटकर अपने साथ ले आये लेकिन उसे रत्नपुर से आगे नहीं ले जा सके और रत्नपुर में ही स्थापित कर दिये।
सरगुजा में आज भी सिरकटी महामाया देवी की मूर्ति है जिसमें प्रतिवर्ष मोम (अथवा मिट्टी) का सिर बनाया जाता है। रत्नपुर में नवरात्र बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहां आज भी हजारों मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित की जाती है। एक अन्य किंवदंति में राजा रत्नदेव शिकार करते रास्ता भटककर यहां के जंगल में आ गये और एक पेड़ की टहनी में रात गुजारी। रात्रि में उन्हें पेड़ के नीचे महामाया देवी का दरबार देखने को मिला। बाद में उन्हें स्वप्नादेश हुआ कि यहां अपनी राजधानी बनाओ। तब राजा रत्नदेव से यहां अपनी राजधानी बसायी और रत्नपुर नाम दिया। प्राचीन काल में यहां नरबलि देने की प्रथा थी जिसे राजा बहरसाय ने बंद करा दिया। लेकिन पशुबलि आज भी दी जाती है।
बस्तर में दंतेश्वरी देवी की शोभायात्रा:-
बस्तर का दशहरा अन्य स्थानों से भिन्न होता है क्योंकि यहां दशहरा में दशानन रावण का वध नहीं बल्कि बस्तर की अधिष्ठात्री दंतेश्वरी माई की विशाल शोभायात्रा निकलती है। दशहरा आमतौर पर अयोध्यापति राजा राम की रावण के उपर विजय का पर्व के रूप में मनाया जाता है लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं होता। वास्तव में बस्तर का ऐतिहासिक दशहरा यहां के राजवंश की गौरवगाथा का जीवन्त दस्तावेज है। ऐतिहासिक दस्तावेज से पता चलता है कि यहां का दशहरा राजधानी का आयोजन रहा है। इस राज्योत्सव का उल्लेख प्रथम काकतीय नरेश अन्नमदेव (1313 ई.) से ही मिलता है। राजा अन्नमदेव अपनी विजययात्रा के दौरान चक्रकोट (बस्तर का प्राचीन नाम) की नलवंशीय राजकुमारी चमेली बाबी पर मुग्ध हो गये। उन्होंने राजकुमारी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा जिसे राजकुमारी ने अस्वीकार कर दिया, यही नहीं बल्कि राजा अन्नमदेव के विरूद्ध सैन्य संचालन करतेी हुई वीरगति को प्राप्त हुई। इस घटना का राजा के उपर गहरा प्रभाव पड़ा…और उन्होंने चमेली बाबी की स्मृति में नारंगी नदी के जल में पुष्प प्रवाहित करने की परंपरा शुरू की। कालान्तर में यह दशहरा की एक अनिवार्य परंपरा बन गयी। आज भी इसका निर्वहन किया जाता है। राजाओं के साथ जहां उनकी राजधानियां बदलीं वही दशहरा उत्सव के स्वरूप में भी परिवर्तन आता गया।
बस्तर की अराध्य दंतेश्वरी माई आज अवश्य है लेकिन वास्तव में वह राजा की ईष्ट देवी के रूप में पूजित होती रहीं हैं। नवरात्र में बस्तर के राजा दंतेश्वरी माई के मंदिर में पुजारी के रूप में नौ दिन रहकर शक्ति साधना किया करते थे। जो देवी राजा की ईष्ट हो वह बस्तरांचल में पूजित न हो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। यही कारण है कि आज दंतेश्वरी माई का बस्तरांचल में विशेष स्थान है। बस्तर की ग्राम देवियों में मावली देवी, हिंगलाजिन, परदेसिन, तेलिन, करनकोटिन, बंजारिन, डोंगरी माता और पाट देवी प्रमुख हैं।
बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर नगर की परिक्रमा करने वाला विशाल रथ का परिचालन बस्तर दशहरा का प्रमुख आकर्षण होता है। प्राचीन काल में यह रथ 12 पहियों का हुआ करता था लेकिन आगे चलकर इसके परिचालन में असुविधा होने लगी जिससे राजा वीरनारायण के शासनकाल (1538-1553 ई.) में इसे आठ तथा चार पहिये वाले दो रथ में निकाला जाने लगा। दशहरा उत्सव में रथयात्रा की शुरूवात राजा पुरूषोत्तमदेव के शासनकाल (1407-39 ई.) में हुई। उन्होंने लोट मारते हुए जगन्नाथ पुरी की यात्रा पूरी की थी जिससे प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ के आदेशानुसार वहां के पुजारी ने राजा को एक रथचक्र प्रदान कर उसे रथपति की उपाधि प्रदान की थी। उन्होंने अपने राज्य में रथयात्रा का आयोजन इसी रथचक्र प्राप्ति के बाद शुरू की थी।
जगन्नाथपुरी की रथयात्रा की तर्ज में उन्होंने बस्तर में गोंचा परब और नवरात्र के बाद दशहरा की उत्सव शुरू की। दशहरा की शुरूवात अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से हो जाती है। इस दिन ब्राह्मणों को बुलाकर देवी देवताओं की पूजा कराये जाते हैं। यह सप्तशती पाठ, बगलामुखी पाठ, हनुमान चालीसा पाठ, विष्णु पाठ के रूप में पूरे नवरात्र में चलता है। सीरसार चैंक में जोगी बिठाई की रस्म होती है। हलबा जाति का आमाबाल गांव का एक व्यक्ति जोगी के रूप में बैठता है। लगभग दस दिनों तक यह व्यक्ति फलाहार करके उत्सव की निर्विघ्न समाप्ति के लिए कामना करता रहता है। नवमीं को जोगी उठाई होती है। जोगी बिठाई के दूसरे दिन से फूलरथ परिक्रमा प्रारंभ करता है। फूलों से अलंकृत होने के कारण यह फूलरथ कहलाता है। भतरा जाति के लोग इस रथ को चुराकर कुम्हड़ाकोट ले जाते हैं। यहीं राजा नवाखाई की शुरूवात करता है। 1898 ई. में इस प्रथा को बंद कर दिया गया।
फूल रथ में राजा बैठकर राजा मावलीगुड़ी से जगन्नाथ गुड़ी तक जाता था। अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से षष्ठी तक राजा कभी नीला पीताम्बर और गले में दुपट्टा डालकर और कभी पूरे शरीर में चंदन लगाकर और हाथ, गला तथा सिर में फूलों की माला डालता था लेकिन इस दौरान वे आभूषण धारण नहीं करते थे। राजा सरस्वती पूजा करते थे। प्रातःकाल राजा ब्राह्मणों के पास देवपाठ सुनने के लिये बैठते थे। फिर मावली डोली अथवा दंतेश्वरी डोली रात्रि नौ बजे आती थी जिसे दंतेवाड़ा से लाया जाता था। माता की सवारी का स्वागत राजा स्वयं अपने कर्मचारियों और सेनाओं के साथ करते थे। इस अवसर पर प्रजा अपनी कला का प्रदर्शन करके पुरस्कृत होते थे।
जब तक दंतेश्वरी माई जगदलपुर में रहते थे, राजा स्वयं उनकी पूजा-अर्चना करते थे। प्रतिदिन बकरा, भैंसा, मुर्गा आदि की बलि दी जाती थी। इस अवसर पर राजा अपनी तलवार की भी पूजा किया करता था। अंतिम क्रिया के रूप में दशहरा पर्व सम्पन्न होता था जिसमें दंतेश्वरी माई की विशाल शोभायात्रा निकाली जाती थी। समूचे बस्तर के ग्रामीण, जमीदार और अन्य ओहदेदार शामिल होते थे। सभी दंतेश्वरी माई की रथ को खींचकर पुण्य के भागीदार बनने को लालायित रहते थे। महिलाएं सुंदर वस्त्राभूषण से सुसज्जित होकर अपने अपने घरों की छतों से इस दृश्य को देखकर आनंदित होती थीं। अन्यान्य महिलाएं इस शोभायात्रा में शामिल भी होती थीं।
काछन गादी, बस्तर दशहरा की एक प्रमुख रस्म है। यह दशहरा का एक प्रारंभिक विधान है। इसके द्वारा युद्ध की देवी काछन माता को तांत्रिक अनुष्ठान के द्वारा जगाया जाता है। कांटों की सेज पर एक महार कन्या को बिठाया जाता है। यहीं पर से वह कन्या दशहरा उत्सव मनाने की घोषणा करती है। पथरागुड़ा के पास जेल परिसर से लगा काछन देवी की गुड़ी है। यहीं पर यह उत्सव होता है। सुप्रसिद्ध साहित्यकार लाला जगदलपुरी के अनुसार हरिजनों की देवी काछन देवी को बस्तर के राजाओं द्वारा सम्मान देना इस बात की पुष्टि करता है कि वे इस राज्य में अपृश्य नहीं थे। इसी प्रकार आपसी सहयोग से विशाल रथ का निर्माण, उसके लिए लकड़ी काटकर संवरा जाति के लोग जंगलों से लाकर करते हैं। इससे उनकी राजा और इस उत्सव के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है। दशहरा का प्रमुख आकर्षण मुरिया दरबार होता था। कदाचित मुरिया जाति की दरबार में ऊंचा स्थान था। दरबार का मुखिया राजा होता था। इस दरबार में राजा अनेक विषयों पर चर्चा करके आदेश जारी करता था और मुरिया इस आदेश को लेकर साल भर के लिए दंतेश्वरी माई से वर्ष भर राज्य में खुशहाली के लिए प्रार्थना कर नई उमंग, नई जागृति और आत्म विश्वास लिए आदिवासी जन अपने गांवों को लौटते हैं।
शिवरीनारायण में गादी पूजा और विजियादशमी:-
छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक और धार्मिक तीर्थ शिवरीनारायण में दो प्रकार का दशहरा मनाया जाता है। नगर के उत्साही नवयुवकों के द्वारा मेला ग्राउंड में जहां रावण की मूर्ति की स्थापना कर श्रीराम लक्ष्मण और हनुमान की शोभायात्रा निकालकर रावण का वध किया जाता है, वहीं मठ के महंत की बाजे-गाजे के साथ शोभायात्रा निकाली जाती है। इस शोभायात्रा में तलवारबाजी और आतिशबाजी की धूम होती है जो जनकपुर जाकर सोनपत्ती के पेड़ की पूजा-अर्चना करके मठ लौट आती है और मठ के बाहर स्थित गादी चैरा में महंत के द्वारा हवन-पूजन की जाती है। इस अवसर पर मठ के साधु संत और नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित होते हैं।
हवन पूजन के उपरांत महंत गादी चैरा में विराजमान होते हैं। उस समय सभी उन्हें यथा शक्ति भेंट देते हैं। ऐसी किंवदंति है कि यह प्राचीन काल में दक्षिणापथ और जगन्नाथ पुरी जाने का मार्ग था। लोग इसी मार्ग से जगन्नाथ पुरी और दक्षिण दिशा में तीर्थ यात्रा करने जाते थे। उस समय यहां नाथ संप्रदाय के तांत्रिक रहते थे और यात्रियों को लूटा करते थे। एक बार आदि गुरू दयाराम दास तीर्थाटन के लिए ग्वालियर से रत्नपुर आए। उनकी विद्वता से रत्नपुर के राजा बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपना गुरू बनाकर अपने राज्य में रहने के लिए निवेदन किया। रत्नपुर के राजा शिवरीनारायण में तांत्रिकों के प्रभाव और लूटमार से परिचित थे। उन्होंने स्वामी दयाराम दास से तांत्रिकों से मुक्ति दिलाने का अनुरोध किया। आदि स्वामी दयाराम दास जी शिवरीनारायण गये। वहां उन्हें भी तांत्रिकों ने लूटने का प्रयास किया मगर वे सफल नहीं हुए, उनकी तांत्रिक सिद्धि स्वामी जी के उपर काम नहीं की।
तांत्रिकों ने स्वामी दयाराम दास को शास्त्रार्थ करने के लिए आमंत्रित किया जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया और फिर दोनों के बीच शास्त्रार्थ हुआ जिसमें तांत्रिकों की पराजय हुई और जमीन के भीतर एक चूहे के बिल में प्रवेश कर अपनी जान की भीख मांगने लगे। स्वामी जी ने उन्हें जमीन के भीतर ही रहने की आज्ञा दी और उनकी तांत्रिक प्रभाव की शांति के लिए प्रतिवर्ष माघ शुक्ल त्रयोदस और विजयादशमी (दशहरा) को पूजन और हवन करने का विधान बनाया। आज भी शिवरीनारायण में शबरीनारायण मंदिर परिसर में दक्षिण द्वार के पास स्थित एक गुफानुमा मंदिर में नाथ सम्प्रदाय के तांत्रिक गुरू कनफड़ा और नगफड़ा बाबा की पगड़ी धारी मूर्ति स्थित है। साथ ही बस्ती के बाहर एक नाथ गुफा भी है। शिवरीनारायण में 9वीं शताब्दी में निर्मित और नाथ सम्प्रदाय के कब्जे में बरसों से रहे मठ में वैष्णव परंपरा की नींव डाली।
शिवरीनारायण के इस मठ के स्वामी दयाराम दास पहले महंत हुए। तब से आज तक 14 महंत हो चुके हैं और 15 वें महंत राजेश्री रामसुंदरदास जी वर्तमान में हैं। इस मठ के महंत रामानंदी सम्प्रदाय के हैं। जिस स्थान में दोनों के बीच शास्त्रार्थ हुआ था वहां पर एक चबुतरा और छतरी बना है। बरसों से प्रचलित इस पूजन परंपरा को ‘‘गादी पूजा‘‘ कहा गया। क्योंकि पूजन और हवन के बाद महंत उसके उपर विराजमान होते हैं और नागरिक गणों द्वारा गादी पर विराजित होने पर महंत को श्री फल और भेंट देकर उनका सम्मान किया जाता है। इस परंपरा के बारे में कोई लिखित दस्तावेज नहीं है मगर महंती सौंपते समय उन्हें मठ की परंपराओं के बारे में जो गुरू मंत्र दिया जाता है उनमें यह भी शामिल होता है। इस मठ में जितने भी महंत हुए सबने इस परंपरा का बखूबी निर्वाह किया है। आज भी यह परंपरा निभायी जाती है।
लेखक वरिष्ठ साहित्यकार एवं लोक संस्कृति के जानकार हैं।