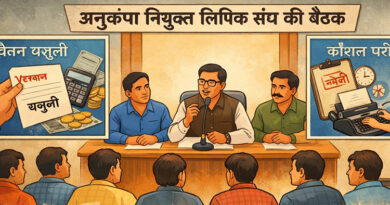भारत में लोकतंत्र की जड़ें पाताल से भी गहरी : अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस

हम इतिहास देखें तो भारत में लोकतंत्र की अवधारणा प्राचीन काल से ही दिखाई देती है। भारत को लोकतंत्र की जननी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसकी जड़ें हमें ऐतिहासिक प्रमाणों और परंपराओं में दृष्टिगोचर होती हैं। लोकतंत्र की परिभाषा व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और भागीदारी पर आधारित है और यदि हम मानव सभ्यता के आरंभिक चरणों को देखें तो भारत ही वह भूमि है, जहाँ इसके अंकुर सबसे पहले फूटे। प्राचीन भारत के समाज में सत्ता का केन्द्रीकरण कम और सामूहिक निर्णय की परंपरा अधिक दिखाई देती है। यही कारण है कि यहां की सांस्कृतिक और राजनीतिक धारा को लोकतंत्र का आरंभिक रूप माना जाता है।
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी नगर सभ्यताओं का उदय लगभग 4500 वर्ष पूर्व हुआ। इन नगरों की संरचना और संगठन देखकर विद्वान यह मानते हैं कि यहां शासन व्यवस्था सामूहिक थी। योजनाबद्ध सड़कों का जाल, सार्वजनिक स्नानागार, जल निकासी प्रणाली और अनाज भंडारण जैसी व्यवस्थाएं बताती हैं कि लोग सामूहिक हित को प्राथमिकता देते थे। आश्चर्य की बात यह है कि अब तक इन स्थलों से किसी शाही महल या विशाल राजसिंहासन के अवशेष नहीं मिले। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यहां सत्ता किसी एक शासक वर्ग के पास केंद्रित नहीं थी, बल्कि समाज का संचालन पंचायत जैसे किसी संस्था से होता होगा। उपलब्ध प्रमाण इस ओर संकेत करते हैं कि हड़प्पा के लोग सामूहिक जीवन जीते थे और सार्वजनिक निर्णय को महत्व देते थे। यह लोकतंत्र का एक प्रारंभिक रूप था, जो बाद में और परिपक्व होता गया।
वैदिक काल में लोकतंत्र के स्वरूप और स्पष्ट हो जाते हैं। ऋग्वेद और अथर्ववेद जैसे ग्रंथों में ‘सभा’ और ‘समिति’ का उल्लेख मिलता है। ये निकाय मात्र सलाहकार संस्थाएं नहीं थे, बल्कि राजा की शक्ति को नियंत्रित करने वाले निकाय थे। सभा स्थायी परिषद थी जिसमें विद्वान और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते थे। समिति बड़ी सभा होती थी जिसमें जनता की राय शामिल होती थी और राजा को अपनी नीतियों के लिए जनता की स्वीकृति लेनी पड़ती थी। यही वह परंपरा है जिसने यह स्थापित किया कि सत्ता शासक की नहीं बल्कि जनता की है और राजा जनता का सेवक है। इतिहासकार के.पी. जयसवाल और अन्य विद्वानों ने स्पष्ट किया है कि इन निकायों का प्रभाव इतना था कि राजा को शपथ लेनी पड़ती थी कि वह गरीबों और वंचितों के कल्याण के लिए काम करेगा। इसका अर्थ है कि प्राचीन भारत में लोकतंत्र केवल राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं बल्कि नैतिकता और सामाजिक कर्तव्य का आधार भी था।
महाजनपद काल में जब बड़े-बड़े जनपद और राज्यों का गठन हुआ तब लोकतंत्र और भी संगठित रूप में सामने आया। इस काल में वज्जी और मल्ल जैसे गणराज्य अस्तित्व में आए। वैशाली स्थित वज्जी गणराज्य उस समय का एक अद्वितीय प्रयोग था। यहां 7707 प्रतिनिधियों की सभा होती थी और निर्णय मतदान के आधार पर होते थे। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिब्बाण सुत्त में बुद्ध ने वज्जियों के सात कल्याणकारी सिद्धांत बताए हैं, जिनमें नियमित सभाएं करना, सामूहिक निर्णय लेना और नियमों का पालन करना प्रमुख हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि यहां लोकतांत्रिक जीवन पद्धति स्थापित थी।
इसी प्रकार मल्ल गणराज्य में भी निर्णय कुलीनों की सभा द्वारा होते थे। यद्यपि ये गणराज्य आज के आधुनिक लोकतंत्र की तरह सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित नहीं थे और इनमें महिलाओं तथा दासों की भागीदारी नहीं थी, फिर भी ये उस युग के किसी भी अन्य समाज से अधिक लोकतांत्रिक थे। यूनान के एथेंस का लोकतंत्र जहां सीमित दायरे में था, वहीं भारत के गणराज्यों ने अधिक विस्तृत और संगठित रूप में लोकतंत्र को अपनाया।
बौद्ध और जैन परंपराओं ने लोकतंत्र को सामाजिक और धार्मिक जीवन का हिस्सा बना दिया। बौद्ध संघों में निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे और मतदान की विधियों का विस्तार से वर्णन विनय पिटक में मिलता है। हाथ उठाकर, गुप्त मतपत्र या आपस में बातचीत करके निर्णय लेना, ये सभी लोकतांत्रिक तरीके थे जिनका पालन संघ के साधु करते थे। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने तो यहां तक कहा था कि बौद्ध संघों की कार्यप्रणाली आधुनिक भारतीय संसद से मिलती-जुलती है। इसी तरह जैन मठों में भी प्रत्येक साधु-साध्वी को अपने विचार रखने का अवसर मिलता था और सामूहिक निर्णय का सम्मान होता था।
मध्यकालीन भारत में भी लोकतंत्र की परंपरा जीवित रही। चोल साम्राज्य के समय का उथिरमेरुर शिलालेख इसका प्रमाण है। इस शिलालेख में ग्रामसभा के चुनाव की पूरी प्रक्रिया दर्ज है। इसमें यह उल्लेख मिलता है कि किस प्रकार गुप्त मतदान से समितियों का चुनाव किया जाता था और चुने जाने वाले व्यक्ति के लिए क्या योग्यताएं अनिवार्य थीं। यह न केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था का बल्कि अत्यंत परिष्कृत चुनावी प्रणाली का प्रमाण है। इसके अलावा 12वीं शताब्दी में बसवन्ना द्वारा कर्नाटक में स्थापित अनुभव मंटप एक ऐसा मंच था, जहां जाति, वर्ग और लिंग की परवाह किए बिना सभी लोग खुलकर अपनी बात रखते थे। इस अनुभव मंटप को लोकतांत्रिक विमर्श का सबसे जीवंत उदाहरण माना जा सकता है।
जब हम इन प्रमाणों को एक साथ देखते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि लोकतंत्र का वास्तविक उद्गम भारत ही है। यूनान का एथेंस लोकतंत्र ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में सामने आया, लेकिन भारत में सभा-समिति और गणराज्य उससे बहुत पहले अस्तित्व में थे। यहां लोकतंत्र केवल राजनीतिक व्यवस्था तक सीमित नहीं था बल्कि यह समाज, धर्म और संस्कृति का हिस्सा था। यह बात भारत को विश्व में अद्वितीय बनाती है और यही कारण है कि भारत को लोकतंत्र की जननी कहना उचित है।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने लोकतांत्रिक परंपरा को आधुनिक रूप में पुनः स्थापित किया। 26 जनवरी 1950 को लागू हुए संविधान ने भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। यह संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है और इसमें सार्वभौमिक मताधिकार, मौलिक अधिकार और स्वतंत्र न्यायपालिका जैसी विशेषताएं शामिल हैं। भारत का लोकतंत्र आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां 90 करोड़ से अधिक मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं।
इस यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारत में लोकतंत्र कोई आयातित विचार नहीं था। यह भारत की मिट्टी में हजारों वर्षों से मौजूद था। हड़प्पा की नगरीय सभ्यता, वेदिक काल की सभा-समिति, वैशाली का वज्जी गणराज्य, बौद्ध संघों की लोकतांत्रिक परंपरा, उथिरमेरुर के शिलालेख और अनुभव मंटप आदि इस बात का प्रमाण हैं कि भारत ने लोकतंत्र को न केवल जन्म दिया बल्कि इसे निरंतर पोषित भी किया।
आज जब हम भारत के लोकतंत्र को उसकी चुनौतियों और उपलब्धियों के साथ देखते हैं तो यह स्मरण करना आवश्यक है कि इसकी जड़ें कितनी गहरी और प्राचीन हैं। यह वह परंपरा है जिसने भारत को एक ऐसी भूमि बनाया जहाँ सत्ता जनता से निकलती है और जनता के लिए ही कार्य करती है। इसलिए यह ऐतिहासिक सत्य है कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें पाताल से भी गहरी हैं।