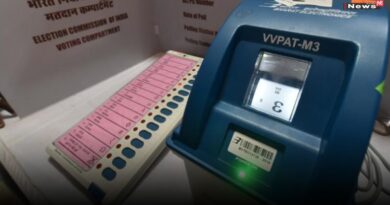भारत में गाणपत्य परंपरा और गणेश उपासना का सांस्कृतिक विस्तार

भारत की प्राचीन धार्मिक परम्परा में भगवान गणेश एक ऐसे देवता हैं जिनका प्रभाव हर युग में देखा जा सकता है। इन्हें विघ्नहर्ता, बुद्धि और विवेक के दाता तथा शुभ कार्यों के आरंभकर्ता के रूप में सम्मानित किया जाता है। आज भी परम्परा है कि किसी भी नये कार्य के आरंभ को श्रीगणेश करना कहा जाता है। गणेश विघ्नहर्ता के रुप में किसी भी कार्य के आरंभ में पूजा जाता है। लोक संस्कृति में सबसे प्रसिद्ध और प्रथम पूजित देवता के रुप में गणेश लोक में स्थापित हैं
गणेश केवल पूजा-पद्धति के देवता नहीं, बल्कि भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी आधार स्तंभ हैं। गाणपत्य सम्प्रदाय ने गणेश को सर्वोच्च देवता के रूप में स्वीकार किया यह सम्प्रदाय भारतीय धर्म और संस्कृति की विविधता में एक विशिष्ट स्थान रखता है। इस सम्प्रदाय के विकास की यात्रा वैदिक काल से लेकर मध्यकाल और आधुनिक युग तक सतत रही है। भारत के अन्य प्रदेशों सहित छत्तीसगढ़ में भी इस परंपरा के सशक्त प्रमाण आज भी विद्यमान हैं, जो यह दर्शाते हैं कि गणेश की उपासना ने यहां की संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया।
वैदिक काल में गणपति की अवधारणा
गणेश की जड़ें वैदिक साहित्य तक जाती हैं। ऋग्वेद (2.23.1) में ‘गणानां त्वा गणपतिम्’ मंत्र मिलता है। यद्यपि यह ब्रह्मणस्पति अथवा इंद्र की ओर संकेत करता है, परंतु बाद के काल में व्याख्याकारों ने इसे गणेश से जोड़ा। ‘गणपति’ का शाब्दिक अर्थ है ‘गणों का स्वामी’। ‘गण’ यहाँ समुदाय या समूह को इंगित करता है, और ‘पति’ उनके नायक को। इस प्रकार गणपति की अवधारणा मूलतः नेतृत्व और संगठन की रही। वैदिक युग में गणेश को ‘विनायक’ भी कहा गया, जिसका संबंध बाधाओं को नियंत्रित करने वाली शक्तियों से है। मानव गृह्यसूत्र में शालकटंक, कुष्माण्डराजपुत्र, उस्मित और देवयजन चार विनायकों का उल्लेख है, जिन्हें गणेश की पूर्ववर्ती अवधारणा माना जाता है।
पुराणिक साहित्य और गणेश की प्रतिष्ठा
पौराणिक ग्रंथों ने गणेश की पूजा को सर्वाधिक लोकप्रिय बनाया। मैत्रायणी संहिता में ‘एकदन्ताय विद्महे’ गणेश गायत्री मंत्र मिलता है, जबकि गणपत्यर्थर्वशीर्ष में गणेश को परब्रह्म के रूप में वर्णित किया गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में ‘ग’ को ज्ञान, ‘ण’ को मोक्ष और ‘पति’ को परमेश्वर से जोड़ा गया, जिससे गणपति का अर्थ ही सर्वोच्च देवता हुआ। विष्णुधर्मोत्तर पुराण में गणेश को चतुर्भुज गजमुख देवता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिनके हाथों में शूल, परशु, अक्षमाला और मोदक पात्र रहते हैं।
महाभारत में गणेश का उल्लेख व्यास के महाकाव्य लेखक के रूप में मिलता है। यह प्रसंग, यद्यपि बाद के काल का माना जाता है, फिर भी इसने गणेश को विद्या और लेखन से जोड़ दिया। वराह पुराण और ब्रह्म पुराण में गणेश जन्म की कथाएं विविध रूपों में मिलती हैं। एक कथा में पार्वती जी द्वारा उबटन से गणेश के पुतले का निर्माण हुआ और फ़िर प्राण डाले गये, तो दूसरी में परशुराम के प्रहार से उनका एक दांत टूटकर ‘एकदंती’ नाम मिलता है। इन कथाओं ने गणेश को विघ्नहर्ता और शुभारंभ देवता के रूप में स्थापित कर दिया।
मूर्तिकला और गणेश की प्रारंभिक प्रतिमाएं
गणेश की सबसे प्राचीन मूर्तियां ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी की मानी जाती हैं। मथुरा से प्राप्त प्रतिमाओं में उन्हें दो भुजाओं वाले रूप में दर्शाया गया है, जहां वे मोदक पात्र लिए हुए हैं। गुप्तोत्तर काल में गणेश प्रतिमाओं का निर्माण व्यापक रूप से हुआ और वे शैव परिवार तथा नवग्रहों के साथ मंदिरों में स्थापित होने लगे। वराहमिहिर की बृहत्संहिता में गणेश को एकदंती, लंबोदर और गजमुख रूप में वर्णित किया गया है। इस काल तक गणेश की मूर्तियां स्थानक, आसनस्थ और नृत्यरत मुद्राओं में बनने लगीं।
छत्तीसगढ़ में गाणपत्य परंपरा का विकास
छत्तीसगढ़ गाणपत्य सम्प्रदाय के पुरातात्विक प्रमाणों से समृद्ध है। बिलासपुर जिले के ताला (अमेरीकापा) स्थित देवरानी मंदिर में पांचवीं-छठी शताब्दी की गणेश प्रतिमा मिली है, जिसमें वे दांत पकड़े और मोदक पात्र लिए दिखते हैं। बलौदाबाजार के पलारी में सिद्धेश्वरी मंदिर में नृत्यरत गणेश की प्रतिमा सातवीं-आठवीं शताब्दी की है। मल्हार संग्रहालय में दशभुजी नृत्यरत गणेश की प्रतिमाएं संरक्षित हैं।
राजनांदगांव के घटियारी और राजिम के रामचंद्र मंदिर में नौवीं-दसवीं शताब्दी की अष्टभुजी प्रतिमाएं हैं। दंतेवाड़ा के ढोलकल में ग्यारहवीं शताब्दी की प्रसिद्ध गणेश प्रतिमा स्थापित है, जहां वे पर्यकासन में परशु और मोदक के साथ विराजमान हैं। बस्तर के बारसूर में गणेश मंदिर और विशाल प्रतिमाएं इस परंपरा के उत्कर्ष को दर्शाती हैं।
कलचुरि शासकों के अभिलेख भी गाणपत्य परंपरा की पुष्टि करते हैं। पृथ्वीदेव द्वितीय के रतनपुर शिलालेख में गजमुख गणेश की स्तुति है, जबकि जाजल्लदेव द्वितीय के मल्हार शिलालेख में गणेश की सूंड की रक्षा की कामना की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि इस काल में गणेश न केवल धार्मिक बल्कि राजनीतिक-सांस्कृतिक जीवन का भी हिस्सा थे।
भारत में गाणपत्य सम्प्रदाय का विस्तार
भारत में गाणपत्य सम्प्रदाय छठी से नौवीं शताब्दी में उभरकर दसवीं शताब्दी में चरम पर पहुंचा। महाराष्ट्र इसका प्रमुख केंद्र रहा। यहां मोरया गोसावी जैसे संतों ने 14वीं शताब्दी में इसे लोकप्रिय बनाया। मोरगांव मंदिर और चिंचवाड़ समाधि इसके केंद्र बने। इस सम्प्रदाय में महा, हरिद्र, स्वेत, नवनीत, उच्छिष्ट और संतान छह उपसम्प्रदाय थे जो गणेश की विभिन्न रूपों की आराधना करते थे।
आदि शंकराचार्य ने पंचायन पूजा में गणेश को शामिल कर उन्हें शैव, वैष्णव, शाक्त, सौर और गाणपत्य परंपराओं में समन्वयकारी स्थान दिया। गणेश पुराण और मुद्गल पुराण ने गणेश को पंचदेवों में स्थापित कर दिया।
क्षेत्रीय विविधताएं और सांस्कृतिक प्रभाव
उत्तर भारत में गणेश पूजन ने स्कंद की लोकप्रियता कम होने के बाद स्थान लिया। यहां उन्हें ब्रह्मचारी अथवा सरस्वती-लक्ष्मी के साथ दर्शाया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन और वाराणसी में प्राचीन मंदिर उनके प्रभाव को दर्शाते हैं। दक्षिण भारत में गणेश को प्रथमज और बुद्धिदाता माना गया। तिरुचिरापल्ली का उच्ची पिल्लयार मंदिर और पिल्लैयारपट्टि का कर्पगा विनायक मंदिर इस परंपरा के प्रमाण हैं।
पश्चिम भारत, विशेषकर महाराष्ट्र में, लोकमान्य तिलक ने गणेश चतुर्थी को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़कर इसे जनआंदोलन का स्वरूप दिया। दगड़ुशेठ हलवाई गणपति और अष्टविनायक मंदिर आज भी इस परंपरा के केंद्र हैं। पूर्वी भारत में गणेश को वैष्णव और शाक्त परंपराओं के साथ मिलाकर पूजा जाता है, जहां वे लक्ष्मी और सरस्वती के साथ पूजे जाते हैं।
गणेश की आइकॉनोग्राफी और सांस्कृतिक संदेश
गणेश की प्रतिमाओं में विविधता उनकी पूजा की बहुआयामी प्रकृति को दर्शाती है। वे चतुर्भुज से अष्टादशभुज रूपों तक मिलते हैं, हाथों में परशु, अक्षमाला, मोदक और स्वदंत धारण करते हैं। मूषक वाहन और एकदंती स्वरूप उनकी विशिष्टता है। गणेश सहस्रनाम में उनके हजार नामों का उल्लेख है, जो उनकी व्यापकता का प्रमाण है।
गणेश व्यापारियों और व्यवसायियों के संरक्षक देवता बने। उनकी पूजा ने समाज में संगठन, एकता और शुभारंभ की भावना को मजबूत किया। यही कारण है कि गणेश पूजा नेपाल, श्रीलंका और दक्षिण-पूर्व एशिया तक फैली, परंतु भारत में इसकी मौलिकता अक्षुण्ण रही।
गाणपत्य सम्प्रदाय का इतिहास दर्शाता है कि गणेश की पूजा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का प्रतीक रही है। छत्तीसगढ़ के मंदिरों और प्रतिमाओं से लेकर महाराष्ट्र के संतों और लोकआंदोलन तक, गणेश ने समय के साथ अपने स्वरूप को बदला और लोगों की जरूरतों के अनुरूप ढाला। वे वैदिक काल के विनायक से लेकर पुराणिक गजानन और आधुनिक विघ्नहर्ता तक एक निरंतर यात्रा के प्रतीक हैं।