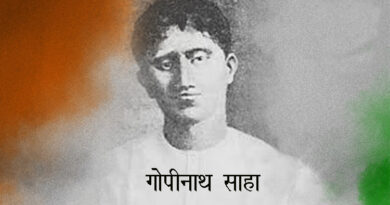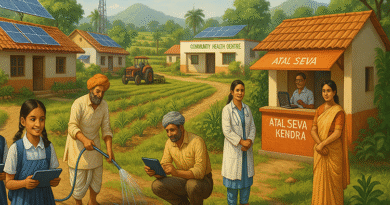भारतीय एक-सींग वाले गैंडे की कहानी, चुनौतियाँ और संरक्षण प्रयास

विश्व गैंडा दिवस हर वर्ष 22 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस केवल एक प्रजाति की सुरक्षा का संदेश नहीं देता, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण की पुकार है। गैंडे, जो धरती पर मौजूद सबसे प्राचीन और अद्भुत जीवों में से एक हैं, आज अस्तित्व के संकट का सामना कर रहे हैं। इनकी पाँच प्रजातियाँ हैं, श्वेत, काला, भारतीय एक-सींग वाला, जावन और सुमात्रन, ये विभिन्न महाद्वीपों में पाई जाती हैं। इनमें से कुछ प्रजातियाँ विलुप्ति के कगार पर हैं, और यही कारण है कि 2010 में WWF-साउथ अफ्रीका ने इस विशेष दिवस की शुरुआत की। एक वर्ष बाद, लीजा जेन कैंपबेल और रिशजा के प्रयासों से यह दिन वैश्विक मंच पर फैल गया और संरक्षण का एक सशक्त प्रतीक बन गया।
गैंडों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अवैध शिकार की है। प्राचीन मान्यताओं और मिथकों के कारण इनके सींगों को औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता रहा है, जबकि वास्तव में ये केवल केराटिन से बने होते हैं, जो हमारे नाखून और बालों का भी आधार तत्व है। इसके बावजूद, अंतरराष्ट्रीय काले बाजार में गैंडे के सींग की भारी मांग है, जिसके चलते इन निर्दोष जीवों का जीवन संकट में पड़ गया है। इसके अतिरिक्त, जलवायु परिवर्तन, बाढ़, अतिक्रमण और घास के मैदानों की गुणवत्ता में गिरावट जैसी समस्याएँ भी इनके अस्तित्व के लिए घातक साबित हो रही हैं।
भारत गैंडे के संरक्षण में विश्व का अग्रणी देश है। यहाँ मुख्य रूप से भारतीय एक-सींग वाला गैंडा पाया जाता है, जिसे ग्रेटर वन-हॉर्न्ड राइनो भी कहा जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा गैंडा है और अपनी विशाल काया, मोटी धूसर-भूरी त्वचा और एकल सींग के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। नर का वजन दो टन से अधिक होता है, जबकि मादा का औसतन डेढ़ टन। गैंडे की दृष्टि कमजोर होती है, परंतु इसकी सूंघने और सुनने की क्षमता अद्भुत है। यह विशालकाय जीव अपनी पूरी ताकत से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है, हालांकि यह गति लंबे समय तक नहीं रह पाती।
ऐतिहासिक रूप से, भारतीय गैंडे का विस्तार पूरे उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप तक था। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र घाटियों से लेकर भारत-म्यांमार सीमा तक यह प्रजाति फैली हुई थी। लेकिन 19वीं शताब्दी तक इनका दायरा सिमटकर केवल तराई और ब्रह्मपुत्र घाटी के घास के मैदानों तक रह गया। वर्तमान में ये भारत और नेपाल के कुल 12 संरक्षित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में असम गैंडों का सबसे बड़ा केंद्र है, जहाँ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान विश्व का सबसे सुरक्षित गैंडा आश्रय स्थल माना जाता है। यहाँ की गिनती 2,600 से अधिक हो चुकी है, जो वैश्विक आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। पश्चिम बंगाल के जलदापारा और गोरुमारा तथा उत्तर प्रदेश के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में भी गैंडे पाए जाते हैं।
आज भारतीय गैंडे की संख्या लगभग 4,075 है, जिनमें से 3,262 भारत में ही हैं। यह संख्या संरक्षण प्रयासों का जीवंत उदाहरण है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जब इनकी संख्या मात्र 200 रह गई थी, तब यह माना जा रहा था कि शायद यह प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। लेकिन समर्पित प्रयासों और कड़े कानूनों की वजह से आज इनकी संख्या में चमत्कारिक वृद्धि हुई है। असम में 1980 के दशक से गैंडों की आबादी 170 प्रतिशत तक बढ़ी है, जो एक बड़ी उपलब्धि है।
गैंडे केवल जीव-जंतु नहीं हैं, बल्कि पारिस्थितिकी के लिए कीस्टोन प्रजाति हैं। वे घास के मैदानों को बनाए रखते हैं, अतिरिक्त वनस्पति को नियंत्रित करते हैं और कई अन्य जीवों के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करते हैं। जब गैंडे कीचड़ में लोटते हैं, तो वे जलस्रोत का निर्माण करते हैं, जो अन्य जानवरों के लिए जीवनदायी सिद्ध होता है। प्रतिदिन ये लगभग 50 किलोग्राम घास खाते हैं और 20 किलोग्राम गोबर से जमीन को उपजाऊ बनाते हैं, जिससे असंख्य कीट-पतंगों और पौधों को सहारा मिलता है। इन्हें संरक्षण देने का अर्थ है पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित करना।
इसके बावजूद चुनौतियाँ खत्म नहीं हुई हैं। अवैध शिकार, निवास स्थान की हानि और मानव-गैंडा संघर्ष अब भी गंभीर समस्या हैं। हर वर्ष कई लोग गैंडे के हमले से मरते हैं और कई गैंडे भी इंसानों के हाथों मारे जाते हैं। यही कारण है कि भारत और नेपाल सरकारों ने, WWF जैसे संगठनों के सहयोग से, कड़े संरक्षण कानून बनाए हैं। असम वन संरक्षण अधिनियम और बंगाल राइनो संरक्षण अधिनियम जैसे कानून इस दिशा में मील का पत्थर साबित हुए हैं।
काजीरंगा का संरक्षण मॉडल विश्वभर के लिए प्रेरणा है। यहाँ न केवल गैंडे, बल्कि बाघ, हाथी और अन्य प्रजातियाँ भी संरक्षित हैं। कई गैंडों को नए क्षेत्रों जैसे मानस और सिकनझार में स्थानांतरित किया गया है, ताकि उनकी संख्या और विविधता सुरक्षित रहे। नेपाल ने भी ‘शून्य शिकार’ की उपलब्धि हासिल की है, जो दर्शाता है कि सामूहिक प्रयास से बड़ी से बड़ी चुनौती का समाधान निकाला जा सकता है।
स्थानीय समुदायों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब लोगों की आजीविका संरक्षण से जुड़ जाती है, तब वे प्रकृति के संरक्षक बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक आजीविका के अवसर दिए गए हैं, ताकि लोग अवैध शिकार की ओर न जाएँ। इको-टूरिज्म भी एक बड़ा साधन है, जिसने लोगों को संरक्षण के लाभ से सीधे जोड़ा है। काजीरंगा का पर्यटन आज विश्व प्रसिद्ध है और इससे स्थानीय लोग आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं।
विश्व गैंडा दिवस हमें यह याद दिलाता है कि गैंडे केवल अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि भविष्य की आवश्यकता भी हैं। यह दिवस मिथकों को तोड़ने, जागरूकता फैलाने और संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाने का अवसर है। यह हम सबके लिए प्रेरणा है कि यदि सही दिशा में प्रयास किए जाएँ तो कोई भी प्रजाति विलुप्ति से बचाई जा सकती है। भारत की सफलता इस बात का प्रमाण है कि इच्छाशक्ति, सामुदायिक सहयोग और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी से बड़े बदलाव संभव हैं।
गैंडे का अस्तित्व हमें यह सिखाता है कि प्रकृति और मानव का रिश्ता परस्पर निर्भरता पर टिका हुआ है। यदि हम गैंडों को बचाते हैं, तो हम वास्तव में अपने पर्यावरण, अपनी जैव विविधता और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करते हैं। यही विश्व गैंडा दिवस का सबसे बड़ा संदेश है कि हम सब मिलकर इन अद्भुत प्राणियों को बचा सकते हैं और धरती को जीवन से भरपूर बनाए रख सकते हैं।