भारत के वैदिक पुनर्जागरण के स्तंभ: श्रीपाद दामोदर सातवलेकर
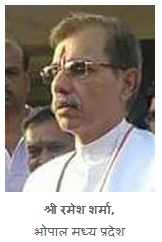 भारत के वैदिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण में अमिट योगदान देने वाले श्रीपाद दामोदर सातवलेकर न केवल एक मूर्धन्य वेदविद थे, बल्कि चित्रकला, राष्ट्रवाद, और शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका प्रभाव अनूठा रहा।
भारत के वैदिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण में अमिट योगदान देने वाले श्रीपाद दामोदर सातवलेकर न केवल एक मूर्धन्य वेदविद थे, बल्कि चित्रकला, राष्ट्रवाद, और शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका प्रभाव अनूठा रहा।
भारत के सांस्कृतिक गौरव का मूल: वेद-वेदांग
भारत राष्ट्र का मूल सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आधार वेद और वेदांग हैं। विदेशी आक्रांताओं ने इन्हें नष्ट-भ्रष्ट करने के अनेक प्रयास किए, लेकिन समय-समय पर ऐसी विलक्षण विभूतियों ने जन्म लिया जिन्होंने इस वैदिक परंपरा को पुनः प्रतिष्ठित किया। श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ऐसी ही एक अद्वितीय विभूति थे।
भारत सरकार ने उन्हें 1968 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया।
प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि
श्रीपाद दामोदर सातवलेकर का जन्म 19 सितंबर 1868 को महाराष्ट्र के सह्याद्रि पर्वत के दक्षिणी छोर स्थित सावंतवाड़ी क्षेत्र के एक छोटे से गांव कोलगांव में हुआ। यह अब रत्नागिरि जिले में आता है।
उनका परिवार ऋग्वैदिक वैदिक परंपरा का पोषक था। पिता दामोदर भट्ट, पितामह अनंत भट्ट, और प्रपितामह कृष्ण भट्ट सभी मूर्धन्य वेदविद थे। अतः श्रीपाद का बचपन वेदों के अध्ययन में ही बीता।
संस्कृत, चित्रकला और शिल्प का समन्वय
8 वर्ष की आयु में उनकी विद्यालयीन शिक्षा प्रारंभ हुई। उन्होंने आचार्य चिंतामणि शास्त्री केलकर से संस्कृत सीखी, और मालवणकर जी से चित्रकला। उनके पिता भी चित्रकला में प्रवीण थे, जिससे यह कला पारिवारिक रूप से आगे बढ़ी।
जल्द ही वे चित्रकला में इतने प्रवीण हो गए कि हैदराबाद में अपनी चित्रशाला स्थापित की। इसके साथ-साथ वे स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय हो गए और वेदों पर आधारित लेखन के माध्यम से समाज जागरण आरंभ किया।
कारावास और नवजीवन की शुरुआत
अपनी क्रांतिकारी वैदिक लेखनी के कारण वे गिरफ्तार हुए और तीन वर्ष जेल में रहे। जेल से छूटने के बाद उनका विवाह वैदिक परिवार की पुत्री सरस्वती देवी से हुआ। विवाह के बाद वे मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने चित्रकला और वेद-वेदांग का अध्ययन जारी रखा।
उन्हें मेयो पदक जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भी दो बार प्राप्त हुए और 1893 में जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई में शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए।
हैदराबाद, आर्य समाज और वैदिक अनुवाद कार्य
1900 में वे फिर हैदराबाद लौटे और देउस्कर जी की सहायता से स्टूडियो बनाया। वहीं उनका संपर्क आर्य समाज से हुआ। उन्होंने “सत्यार्थ प्रकाश”, “ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका” और “योग तत्वादर्श” का मराठी में अनुवाद किया।
उनके तर्क, विश्लेषण और वेदों की गहराई से व्याख्या से समूचा वैदिक समाज प्रभावित हुआ।
विवेक वर्धिनी और स्वाध्याय मंडल की स्थापना
हैदराबाद से निष्कासन के बाद वे हरिद्वार और फिर औंध पहुँचे। यहाँ उन्होंने 1919 में स्वाध्याय मण्डल की स्थापना की और चारों वेदों — ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद — का अनुवाद कार्य आरंभ किया।
उन्होंने हिंदी में मासिक पत्रिका “वैदिक धर्म” (1919) और मराठी में “पुरुषार्थ” (1924) का प्रकाशन भी शुरू किया।
सरल वेदाध्ययन के लिए पुस्तक लेखन
छात्रों और आम पाठकों के लिए उन्होंने संस्कृत स्वयं शिक्षक पुस्तकमाला की रचना की, जिससे वेदों की भाषा को सरल व बोधगम्य बनाया जा सके।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव और स्वतंत्रता आंदोलन
1936 में सतारा में वे डॉ. हेडगेवार से मिले और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। उन्हें औंध रियासत का संघचालक बनाया गया। उन्होंने 16 वर्षों तक शाखाएं प्रारंभ कर कार्य विस्तार किया।
1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वे फिर जेल गए। अस्वस्थता के चलते रिहा होकर वे पूरी तरह वेद-वेदांग के अध्ययन-लेखन में जुट गए।
409 ग्रंथों की रचना और वैदिक भाष्य
उन्होंने कुल 409 ग्रंथों की रचना की, जिनमें सबसे प्रतिष्ठित हैं:
-
ऋग्वेद सुबोध भाष्य (4 खंड)
-
यजुर्वेद सुबोध भाष्य (2 खंड)
-
सामवेद सुबोध अनुवाद
-
अथर्ववेद सुबोध भाष्य (4 खंड)
इसके अतिरिक्त उन्होंने विभिन्न संहिताओं का मूल पाठ भी प्रकाशित किया — जैसे:
-
यजुर्वेदीय काठक, मैत्रायणी, काण्व, तैत्तिरीय संहिताएँ
“वैदिक राष्ट्रगीत” ग्रंथ पर प्रतिबंध
उनका ग्रंथ “वैदिक राष्ट्रगीत”, जो राष्ट्रशत्रु शक्तियों के विनाश हेतु वैदिक मंत्रों का संग्रह था, अंग्रेजी शासन को नागवार गुजरा। इसके प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा और सभी प्रतियाँ जब्त कर नष्ट करने का आदेश हुआ। यह प्रतिबंध स्वतंत्रता के बाद ही हटाया गया।
श्रीपाद दामोदर सातवलेकर का अवसान
उन्हें 9 जून 1968 को पक्षाघात हुआ और 31 जुलाई 1968 को 101 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ।
विरासत और योगदान
श्रीपाद सातवलेकर केवल एक वेदविद नहीं थे, वे राष्ट्रवाणी के प्रचारक, धर्मरक्षक, स्वतंत्रता सेनानी और संघ-संचालक भी थे। उनका योगदान भारत के वैदिक पुनर्जागरण में अद्वितीय है, और सनातन समाज उनके प्रति सदैव ऋणी रहेगा।




