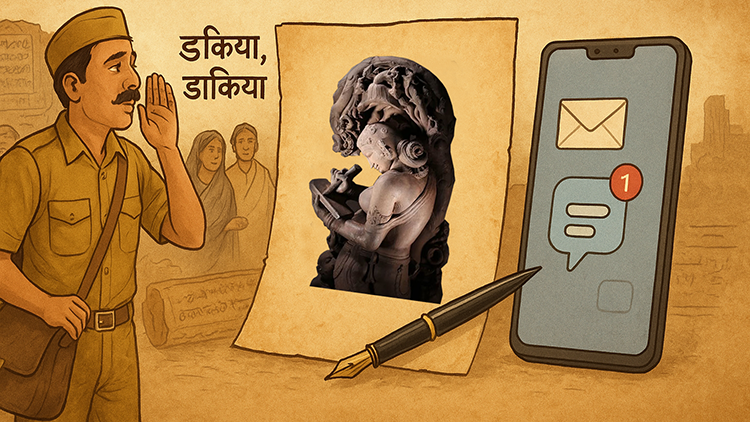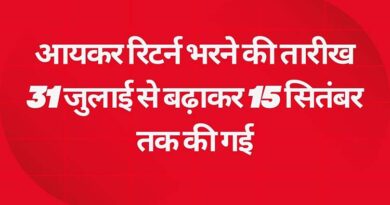खत लिख दे सांवरिया के नाम बाबू

गाँव की गली में जब ‘डाकिया’ ‘डाकिया’ की आवाज गुंजती थी तब सारे काम छोड़कर लोग घरों से बाहर निकलकर देखते थे कि कहीं हमारी कोई चिट्ठी आई होगी। डाकिये का बेसब्री से इंतजार रहता था। तत्कालीन समय में डाकिया ही एक ऐसा व्यक्ति होता था जो सुदूर के समाचार अपनों तक पहुंचाता था। डाकिया ही एक ऐसा व्यक्ति था, जो पत्रों के माध्यम से खुशी और दुख दोनों के संदेश लेकर आता था।
रिश्तेदारों को पत्र लिखे जाते थे, उनके उत्तर आने की प्रतीक्षा बेसब्री से होती थी। तब पत्र लिखना भी एक कला होती थी। अधिक पढे लिखे न होने के कारण लोग पत्र लिखवाने एवं पढवाने के लिए पढे लिखे व्यक्ति ढूंढते थे। पत्र लिखने और पढने वाले की गाँव में बहुत इज्जत होती थी। पत्र का आरंभ ‘यहाँ कुशल है भांति भलाई, वहाँ कुशल राखे रघुराई’ आदि जैसे शब्दों से होता था। कुछ संस्कृत से आरंभ करते थे ‘ अत्र कुशलम तत्रास्तु।’ सबको और सबकी तरफ़ से राम राम लिखा जाता था और अंत में पत्र लेखक अपना नाम भी लिखता था। इन पत्रो में लिखे शब्दों के माध्यम से समाचारों का आदान प्रदान भावनाओं के एक पुल का निर्माण करता था।
भारत में पत्र लेखन का इतिहास प्राचीन है। रामायण एवं महाभारत काल में भी हमें पत्रों के भेजे जाने की जानकारी मिलती है। हरकारे संबंधित तक पत्र पहुंचाते थे और संदेश लेकर भी आते थे। इसके बाद भारत में लेखन का इतिहास सिंदु-सरस्वती सभ्यता में 7000 ईसा पूर्व से शुरू होता है। यहां सारस्वती लिपि के लगभग चार सौ 400 चिह्न सील्स और तांबे की पट्टिकाओं पर मिलते हैं, जो स्वामित्व या व्यापार के लिए इस्तेमाल होते थे। हालांकि, ये पत्र नहीं थे, बल्कि छोटे संदेश या हस्ताक्षर जैसे थे। 1900 ईसा पूर्व सरस्वती नदी के सूखने से सभ्यता पूर्व की ओर स्थानांतरित हुई और 900 ईसा पूर्व, गंगा-यमुना घाटी में ब्राह्मी लिपि उभरी।
पत्र लेखन का सबसे पुराना पुरातात्विक प्रमाण 268-232 ईसा पूर्व अशोक काल में मिलता है, जहां खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपियों में शिलालेख मिलते हैं। अशोक के शिलालेख सार्वजनिक पत्र हैं जो राजाज्ञा के साथ अधिकारियों को निर्देश भी देते थे, जैसे रुपनाथ संस्करण में वितरण के आदेश। ये प्रशासनिक पत्र थे, जो धर्म प्रचार के लिए इस्तेमाल होते थे। ब्राह्मी पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व से दक्षिण भारत में बर्तनों के टुकड़ों पर मिलती है, लेकिन व्यक्तिगत नामों के रूप में, न कि पत्रों के। खरोष्ठी लिपि उत्तर-पश्चिम में कानूनी दस्तावेजों के लिए इस्तेमाल हुई है।
साहित्य में पत्रों का उल्लेख बाद में मिलता है। वेद मौखिक थे, लेकिन दूसरी शताब्दी ईस्वी की याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखित दस्तावेजों को पत्र लेखन का प्रमाण माना गया। प्रेम पत्रों की चर्चा भी होती है। चौथी पांचवीं शताब्दी में कालिदास की विक्रमोर्वशीयम में उर्वशी का भूर्ज पत्र पर प्रेम संदेश लिखना, तमिल सिलप्प आदिकरण में माधवी का ताड़पत्र पर पत्र लिखना और रुक्मिणी का कृष्ण को पत्र लिखना आदि से ज्ञात होता है कि पत्रों का विभिन्न संदर्भों में प्रयोग होता था। खजुराहो मंदिर शिल्प में पत्र लिखती हुई एक विदूषी महिला की मूर्ति विद्यमान है। जो तत्कालीन समय में महिलाओं की विद्वता एवं उच्च शिक्षा को प्रगट करते हुए, सामाजिक स्थिति का प्रमाण है।
मध्यकाल में लेखन शैली और भाषा के विकास के साथ पत्र लेखने के माध्यमों का विकास हुआ। भोजपत्र, ताड़पत्र, कपड़ा तथा तांबे की पट्टियों के साथ बांस की खपच्चियों पर संदेश लिखने साथ ग्रंथ भी लिखे जाने लगे। जिसे हम चिट्ठी कहते है उसका नाम ‘पत्र’ वृक्षों की छाल पर ही लिखे जाने के कारण पड़ा। कागज के अविष्कार के बाद पत्रों का चलन और बढा, जिसका परिष्कृत रुप में आज भी दिखाई देता है। आधुनिक काल में कागज का प्रयोग संदेश भेजने में सरल होने के साथ सहज भी था। कागज का प्रयोग बहुतायत में हुआ।
प्राचीन काल में संवदिया संवदिया होते थे, ये डाकिया का परिष्कृत संस्करण माना जा सकता है, जो अपने मालिक के संदेश को अगले व्यक्ति तक उसी भाव और शब्दों के साथ पहुंचाते थे जिस भाव एवं शब्दों में मालिक ने कहा होता था तथा लौटकर उत्तर भी उसी भाव के साथ सुनाते थे। वर्तमान में द्रुत गति के डिजिटल संसार के विभिन्न मंचों से एक क्लिक पर समाचार और संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। लोग वीडियो कॉल करके प्रत्यक्ष चर्चा कर लेते हैं। इस तरह समय के साथ संदेश भेजने की शैली एवं माध्यमों में बहुत विकास हुआ है। लेकिन अब वो प्रतीक्षा और संबंधों में मिठास नहीं रही, जो होती थी।
हिन्दी सिनेमा भी पत्रों कें छिपी भावनाओ एवं संवेदनाओं से अछूता नहीं रह सका। चिट्ठी, पत्र या संदेश जुड़े भाव भरे गानों की एक विस्तृत शृंखला दिखाई देते हैं। प्रेम की अभिव्यक्ति से लेकर विरह के दर्द तक, और देशभक्ति से लेकर हास्य तक। ये गाने न केवल मनोरंजन प्रदान करते हैं बल्कि उस दौर की सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को भी प्रतिबिंबित करते हैं। अफसाना लिख रही हूं, बड़ी बड़ी पाती लिखवाईयां, दिल की शिकायत नजर की शिकवे, तेरा खत लेके सनम, चंदा रे मोरी पतियां ले जाये, मेरा प्रेम पत्र पढ़कर, खत लिख दे सांवरिया के नाम बाबू, लिखे जो खत तुझे, फूल तुम्हें भेजा है खत में, तेरे खुशबू में बसे खत, चिट्ठी आई है, चिट्ठी है वतन से चिट्ठी आई है, संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए आदि गाने आज भी मन को भिगो देते हैं।
संदेश भेजने के नवीन माध्यमों के आने के कारण नई पीढी पत्र लेखन नहीं जानती। व्यक्तिगत पत्रों से लेकर सरकारी पत्रों के लेखन की शैली भी लगभग समाप्त होने की ओर है। इसके साथ ही डाक विभाग ने ‘तार सेवा’ बंद कर दी। बाकी सेवाएं भी धीरे धीरे बंद हो जाएंगी क्यों अब प्रचलन में नहीं है। अब डाकिया की कोई प्रतीक्षा नहीं करता। डाकिया सिर्फ़ सरकारी पत्र और पत्र पत्रिकाएं ही लेकर आता है। मनीआर्डर का चलन भी डिजिटल पेमेंट ने बंद कर दिया। लेकिन पत्र लेखन फ़िर शुरु होना चाहिए, क्योंकि पत्र इतिहास के अभिलेख हैं, जो सदियों तक अपनी सुगंध बिखेरते हैं। कुछ लोग नॉस्टेल्जिया की तलाश में पत्र लिख रहे हैं, वे पत्र लेखन को जीवित रखना चाहते हैं।
विश्व पत्र लेखन दिवस हर साल 1 सितंबर को मनाया जाता है, यह हमें उस पुरानी परंपरा की ओर लौटने का न्योता देता है जो न सिर्फ शब्दों का आदान-प्रदान था, बल्कि भावनाओं का एक पुल था। इस दिवस की स्थापना 2014 में ऑस्ट्रेलियाई लेखक और फोटोग्राफर रिचर्ड सिम्पकिन ने की थी, जो हस्तलिखित पत्रों की खुशी से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इसे वैश्विक उत्सव बना दिया। ध्यान रहे, पत्र मालवेयर या वायरस नहीं फैलाते, और गोपनीयता बनाए रखते हैं। विश्व पत्र लेखन दिवस हमें प्रोत्साहित करता है कि हम पेन और पेपर उठाएं, और अपनों को भावनाओं और संवेदनाओं का वह स्पर्श दें जो स्क्रीन नहीं दे सकती।

-आचार्य ललित मुनि