समर्पण, सेवा और संस्कार का प्रतीक मालवीयजी का जीवन
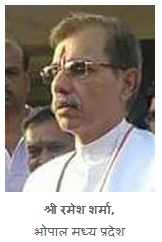 पंडित मदनमोहन मालवीय का नाम आते ही सबसे पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय का चित्र आंखों के सामने उभर आता है। यह केवल एक शैक्षणिक संस्था नहीं, बल्कि भारत की आत्मा और उसकी सांस्कृतिक एकता की मूर्त अभिव्यक्ति है। यह विश्वविद्यालय महामना के उस स्वप्न का साकार रूप है जिसमें उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी, जहाँ शिक्षा केवल ज्ञान का माध्यम न होकर चरित्र निर्माण और राष्ट्रीय पुनर्जागरण का आधार बने। उनकी बहुआयामी प्रतिभा, त्याग और समर्पण ने उन्हें वह गौरव दिलाया जिसे इतिहास ने सदा के लिए “महामना” के नाम से अमर कर दिया।
पंडित मदनमोहन मालवीय का नाम आते ही सबसे पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय का चित्र आंखों के सामने उभर आता है। यह केवल एक शैक्षणिक संस्था नहीं, बल्कि भारत की आत्मा और उसकी सांस्कृतिक एकता की मूर्त अभिव्यक्ति है। यह विश्वविद्यालय महामना के उस स्वप्न का साकार रूप है जिसमें उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी, जहाँ शिक्षा केवल ज्ञान का माध्यम न होकर चरित्र निर्माण और राष्ट्रीय पुनर्जागरण का आधार बने। उनकी बहुआयामी प्रतिभा, त्याग और समर्पण ने उन्हें वह गौरव दिलाया जिसे इतिहास ने सदा के लिए “महामना” के नाम से अमर कर दिया।
पंडित मदनमोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 को प्रयागराज में हुआ। उनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के विद्वान और भगवताचार्य थे, जबकि माता मोनादेवी भारतीय संस्कृति और परंपरा से ओतप्रोत एक आदर्श गृहिणी थीं। परिवार मूल रूप से मालवा क्षेत्र का था, जो मध्यकालीन अशांति के समय प्रयाग आकर बस गया। यही कारण है कि उन्हें “मालवीय” कहा जाने लगा। पारिवारिक वातावरण वैदिक और धार्मिक संस्कारों से भरा था। इसी माहौल में बचपन से ही मदनमोहन के व्यक्तित्व का निर्माण हुआ।
बाल्यावस्था से ही उनमें अद्भुत आत्मविश्वास और गंभीरता झलकती थी। पाँच वर्ष की उम्र में वे पंडित हरदेव धर्मज्ञानोपदेश पाठशाला में पढ़ने लगे और संस्कृत के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा में भी निपुण होते गए। प्रयाग के विद्यालयों में अध्ययन करते हुए उन्होंने “मकरंद” उपनाम से कविताएँ लिखनी शुरू कीं, जो पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती थीं। 1879 में उन्होंने म्योर सेंट्रल कॉलेज से मैट्रिक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया और आगे की पढ़ाई के लिए कलकत्ता पहुँचे। 1884 में बी.ए. परीक्षा में भी प्रथम श्रेणी प्राप्त की। वे विद्वान होने के साथ अत्यंत सादे और अनुशासित स्वभाव के थे। नियमित व्यायाम, संयमित जीवन और सटीक भाषा उनका जीवन नियम था।
उनका व्यक्तित्व जितना सरल था, उतना ही प्रभावशाली भी। बाल्यकाल से ही वे प्रवचन देने लगे थे। सात वर्ष की उम्र में माघ मेले में संस्कृत में प्रवचन देना उनके अद्भुत आत्मविश्वास का प्रमाण था। उनके व्याख्यानों में धर्म, संस्कृति, और समाज के साथ-साथ राष्ट्रीय चेतना की गूंज सुनाई देती थी। प्रारंभ में वे आध्यात्मिक विषयों पर बोलते थे, परंतु धीरे-धीरे उनके भाषणों में राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना गहराने लगी। रॉलेट एक्ट के विरोध में उनका साढ़े चार घंटे का ऐतिहासिक भाषण पूरे देश में प्रसिद्ध हुआ और उनके नेतृत्व की पहचान बन गया।
स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। वे कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे और 1892 के प्रयाग अधिवेशन में उन्होंने भारतीयों के नागरिक अधिकार और सम्मान वृद्धि का प्रस्ताव रखा। यही वह क्षण था जब कांग्रेस ने राजनीतिक चेतना का नया अध्याय शुरू किया। वंदे मातरम् गीत को कांग्रेस अधिवेशनों में गाने की परंपरा भी मालवीयजी ने ही शुरू कराई।
1922 के चौरीचौरा कांड के बाद जब गांधीजी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया, तब आंदोलन में एकता बनाए रखने के लिए मालवीयजी ने देशभर में पदयात्रा की। उस समय वे 61 वर्ष के थे, फिर भी उन्होंने थकान को कभी अपने मार्ग में नहीं आने दिया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में वे जेल गए और नैनी जेल की कठिन परिस्थितियों में भी अपनी साधना और दिनचर्या नहीं छोड़ी।
मालवीयजी राष्ट्र की एकता के पक्षधर थे। वे धार्मिक आधार पर विभाजन या विशेषाधिकार के विरोधी थे। उनका मानना था कि स्वराज्य की प्राप्ति केवल सामूहिक एकता से ही संभव है। कांग्रेस में जब गरम दल और नरम दल के मतभेद बढ़े, तब वे दोनों के बीच सेतु बनकर खड़े हुए। एनी बेसेंट ने उन्हें “भारतीय एकता की सजीव प्रतिमा” कहा था।
मालवीयजी का जीवन राष्ट्र और धर्म के प्रति अटूट समर्पण का उदाहरण था। उनका प्रिय वाक्य था—“प्राण चले जाएं, पर धर्म न जाए।” वे जानते थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता तभी स्थायी होगी जब समाज में सांस्कृतिक और आत्मिक जागृति होगी। इसी सोच से उन्होंने शिक्षा, पत्रकारिता और समाजसेवा तीनों दिशाओं में कार्य किया।
उन्होंने “हिंदुस्तान”, “अभ्युदय”, “लीडर” और “विश्वबंधु” जैसे पत्रों का संपादन किया और पत्रकारिता को राष्ट्र निर्माण का माध्यम बनाया। 1910 में उन्होंने हिन्दी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की और भाषा की सरलता तथा शुद्धता पर जोर दिया। वे मानते थे कि “हिन्दी राष्ट्रीयता की आत्मा है” और एक दिन यह सम्पूर्ण भारत की भाषा बनेगी।
समाज सेवा के क्षेत्र में भी उनका योगदान अमूल्य था। उन्होंने प्रयाग में भारती भवन पुस्तकालय, हिन्दू छात्रालय, मिण्टो पार्क, हरिद्वार में ऋषिकुल, गौरक्षा संस्थाएँ और अनेक सेवा समितियाँ स्थापित कीं। लेकिन उनके जीवन का सर्वोच्च कार्य रहा—काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। यह विश्वविद्यालय उनके दूरदर्शी चिंतन और भारत के भविष्य की सांस्कृतिक परिकल्पना का सजीव प्रतीक है। यहाँ प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक विज्ञान का सुंदर संगम दिखाई देता है। परिसर के मध्य स्थित विश्वनाथ मंदिर भारतीय स्थापत्य और संस्कृति की आत्मा को प्रकट करता है।
महामना का जीवन कर्मयोग का आदर्श था। वे मृदुभाषी, विनम्र और अनुशासित व्यक्ति थे। सत्य, ब्रह्मचर्य, देशभक्ति और आत्मत्याग उनके जीवन के स्तंभ थे। 12 नवंबर 1946 को उन्होंने इस संसार से विदा ली, पर उनका जीवन आज भी राष्ट्र की चेतना में जीवित है। स्वतंत्रता के अट्ठावन वर्ष बाद, 24 दिसंबर 2014 को भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया, युगपुरुष महामना की अमर साधना के प्रति राष्ट्र कृतज्ञ है।




