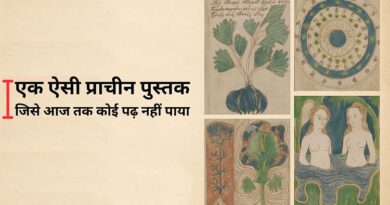जिनके गीतों से छत्तीसगढ़ को मिली सांस्कृतिक पहचान : स्मृति शेष लक्ष्मण मस्तुरिया

(ब्लॉगर एवं पत्रकार )
जिनके लिखे सुमधुर गीतों ने भारत के नक्शे पर छत्तीसगढ़ को एक नई सांस्कृतिक पहचान दी, आज उन्हीं लोकप्रिय कवि और गायक लक्ष्मण मस्तुरिया की पुण्यतिथि है। उन्हें हमारे बीच से गए सात साल बीत गए। आज ही के दिन 3 नवंबर 2018 को वह इस भौतिक संसार से हमेशा के लिए चले गए थे। लेकिन उनकी संगीतमय रचनाएँ और उनकी मधुर आवाज हमारी दुनिया में आज भी मौजूद हैं, जो सुनने वालों के दिल-दिमाग को भावुकता से भर देती हैं।
अपने देश, अपनी धरती, अपनी माटी, अपनी नदी, अपने पंछी, अपने पर्वत, अपने जंगल, अपने खेत, अपने खलिहान, अपने गांव और अपने लोगों की कोमल भावनाओं को शब्द और आवाज देने वालों को समाज अपने दिल में बसा लेता है। फिर चाहे वे कवि हों या गायक। अपनी रचनाओं में, अपनी आवाज में मानव-मन की संवेदनाओं को, लोगों के दुःख-सुख को जगह देने वाले शब्द-शिल्पी और स्वर-साधक ही कला-संस्कृति के जरिए किसी भी राज्य और देश की पहचान बनाते हैं।
अगर किसी कवि में शब्दों के मोतियों के साथ वाणी का माधुर्य भी हो, तो उसका शिल्प और सृजन नदियों के संगम की तरह और भी पावन हो जाता है। लक्ष्मण मस्तुरिया की गिनती भी ऐसे सर्वोत्तम शब्द-शिल्पियों में होती थी, जो पिछले करीब चार दशकों से जारी अपनी काव्य-यात्रा में छत्तीसगढ़ के दिल की धड़कनों को छत्तीसगढ़ के दिल की भाषा — छत्तीसगढ़ी — में आवाज देकर सही मायने में कवि-धर्म का बखूबी पालन कर रहे थे। उन्होंने अपने गीतों को मंच और रंगमंच के साथ-साथ संगीत से भी जोड़ा।
अपनी भौगोलिक और सांस्कृतिक खूबियों से ही कोई भी अंचल देर-सबेर एक राज्य का आकार लेता है। धरती के भूगोल को राज्य और देश के रूप में पहचान दिलाने में साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े कवियों, कलाकारों और शिल्पकारों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आज अगर छत्तीसगढ़ पिछले 25 वर्षों से भारत के छब्बीसवें राज्य के रूप में पहचाना जा रहा है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान लक्ष्मण मस्तुरिया जैसे लोक-प्रिय कवियों का भी है, जिन्होंने राज्य-निर्माण के भी लगभग तीस बरस पहले कवि-सम्मेलनों और सांस्कृतिक मंचों पर छत्तीसगढ़ की माटी का जयगान कर और धरती का जयकारा लगाकर जनता को उसकी आंचलिक अस्मिता और आंतरिक शक्ति का अहसास दिलाया।
लक्ष्मण मस्तुरिया जैसे श्रेष्ठ रचनाकार के गीतों को पढ़ने और उनकी चर्चा करने का एक अपना सुख है, पर इन गीतों की मिठास तो केवल उनकी आवाज में और दूसरे कलाकारों के संगीतमय स्वरों में उन्हें सुनकर ही महसूस की जा सकती है।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के अंतर्गत ग्राम मस्तुरी की माटी में 7 जून 1949 को जन्मे लक्ष्मण महज बाईस साल की उम्र में प्रसिद्ध सांस्कृतिक संस्था ‘चंदैनी गोंदा’ के मुख्य गायक बन चुके थे। दाऊ रामचंद्र देशमुख इसके संस्थापक थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान और आंचलिक स्वाभिमान को देश और दुनिया के सामने लाने के लिए लोक-कलाकारों और कवियों को एक छत के नीचे लाकर दुर्ग जिले के अपने गाँव बघेरा में इसकी बुनियाद रखी थी, जहाँ 7 नवंबर 1971 को अंचल के दूर-दूर से आए हजारों लोगों के बीच इसका पहला प्रदर्शन हुआ।
छत्तीसगढ़ के खेत-खलिहान और मजूर-किसान के जीवन-संघर्ष को गीतों भरी मार्मिक कहानी के रूप में, एक सुंदर और हृदयस्पर्शी गीत-नाट्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए ‘चंदैनी गोंदा’ ने यहाँ की जनता के दिलों में बरसों-बरस राज किया। गणेश उत्सव और दुर्गोत्सव जैसे सार्वजनिक आयोजनों में गाँवों और शहरों में जहाँ भी इसका प्रदर्शन होता, हजारों की संख्या में जनसैलाब उमड़ जाता।
नारायणलाल परमार ने ‘चंदैनी गोंदा’ पर केंद्रित अपने एक आलेख में इसके एक प्रस्तुतिकरण की उद्घोषणा का संदर्भ देकर लिखा है कि यह प्रतीकात्मक रूप से कृषक-जीवन का ही चित्रण है। गेंदे के फूल दो प्रकार के होते हैं — बड़ा गोंदा सिर्फ श्रृंगार के काम आता है, जबकि छोटे आकार के गेंदे को छत्तीसगढ़ी में ‘चंदैनी गोंदा’ कहा जाता है, जो देवी की पूजा में अर्पित किया जाता है। देखा जाए तो गेंदे के फूलों का यह पौधा छत्तीसगढ़ के गाँवों में हर घर के आँगन की शान होता है।
तो इसी ‘चंदैनी गोंदा’ को प्रतीक बनाकर छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक जागरण की एक नयी यात्रा की शुरुआत हुई, जिसके सुंदर और मनभावन गीतों में से अनेक सुमधुर गीत अकेले लक्ष्मण मस्तुरिया ने लिखे थे। ‘चंदैनी गोंदा’ के शीर्षक गीत के रचनाकार थे रविशंकर शुक्ला। उनके अलावा स्वर्गीय कोदूराम ‘दलित’, स्वर्गीय रामरतन सारथी और स्वर्गीय प्यारेलाल गुप्त सहित द्वारिका प्रसाद तिवारी ‘विप्र’, नारायणलाल परमार, पवन दीवान, भगवतीलाल सेन, हेमनाथ यदु, रामेश्वर वैष्णव, मुकुंद कौशल, विनय पाठक, राम कैलाश तिवारी और चतुर्भुज देवांगन जैसे जाने-माने कवियों की रचनाएँ भी ‘चंदैनी गोंदा’ के मंचों पर गूंजा करती थीं।
इस सांस्कृतिक मंच के संगीत निदेशक थे खुमान साव। ग्राम बघेरा में दाऊ रामचंद्र देशमुख का विशाल बाड़ा छत्तीसगढ़ के नए-पुराने कवियों और लोकजीवन में रचे-बसे ग्रामीण कलाकारों का तीर्थ बन चुका था।
अपनी कला-यात्रा के उस प्रारंभिक दौर को याद करते हुए लक्ष्मण मस्तुरिया ने वर्षों पहले एक बार मुझे बताया था —
“देशमुख जी स्वयं महान कला-पारखी थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ के घुमंतू ‘देवार’ समुदाय के लोक-कलाकारों को भी ‘चंदैनी गोंदा’ से जोड़ा। देवार कबीले के अनेक सदस्य बंदरों का नाच दिखाकर कुछ पैसे कमा लिया करते थे। देशमुख जी उन्हें ‘चंदैनी गोंदा’ के जरिए कुछ स्थायित्व देना चाहते थे। उन्होंने उनकी नाचने-गाने की पारंपरिक कला को वर्ष 1974–75 में ‘देवार-डेरा’ के नाम से संस्था बनाकर एक नई पहचान दिलाई।”
देशमुख जी के निर्देश पर लक्ष्मण मस्तुरिया ने इन ‘देवारों’ के बहुत से निरर्थक शब्दों वाले पारंपरिक गीतों को परिमार्जित किया। लक्ष्मण मस्तुरिया ने ‘चंदैनी गोंदा’ के लिए लगभग डेढ़ सौ गीत लिखे। मंच पर इनमें से चालीस–पचास गीतों का ही उपयोग हुआ, जो जनता के दिलों पर छा गए।
सांस्कृतिक जागरण के इस मंच ने कवि लक्ष्मण मस्तुरिया को माटी की महक और मानवीय संवेदनाओं से भरपूर उनके गीतों के जरिए छत्तीसगढ़ में आवाज की दुनिया का नायक भी बना दिया। धरती की धड़कनों से जुड़े उनके इन छत्तीसगढ़ी गानों को जनता ने हाथों-हाथ लिया। आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से जब उनके सुमधुर स्वरों में और उनके सहयोगी कलाकारों की आवाज में इन गीतों का संगीतमय प्रसारण होने लगा, तो ये गीत लोगों की जुबान पर चढ़कर जन-गीत बन गए।
उनका यह गीत आज भी छत्तीसगढ़ की माटी में रचे-बसे हर इंसान को सामूहिकता की भावना में बाँध लेता है और लोग इन पंक्तियों को अनायास गुनगुनाने लगते हैं —
मोर संग चलव रे, मोर संग चलव जी,
ओ गिरे-थके हपटे मन, अऊ परे-डरे मनखे मन,
मोर संग चलव रे, मोर संग चलव जी।
अमरैया कस जुड छाँव म मोर संग बईठ जुड़ालव,
पानी पी लव मै सागर अवं, दुःख-पीरा बिसरा लव।
नवा जोत लव, नवा गाँव बर, रस्ता नवां गढ़व रे!
लक्ष्मण मस्तुरिया का यह गीत वास्तव में समाज के गिरे-थके, ठोकर खाए, भयभीत लोगों को अपने साथ चलने, आम्रकुंज की छाँव में बैठकर शीतलता का अहसास करने, अपनी भावनाओं के सागर से पानी पीकर दुःख-पीरा को भूल जाने और एक नए गाँव के निर्माण के लिए आशा की नई ज्योति लेकर नया रास्ता गढ़ने का आह्वान करता है।
अपने इसी गीत में लक्ष्मण अपनी आवाज में जनता को यह भी संदेश देते हैं —
महानदी मय, अरपा-पैरी, तन-मन धो फरियालव,
कहाँ जाहू बड़ दूर हे गंगा, पापी इहाँ तरव रे,
मोर संग चलव रे, मोर संग चलव जी!
इस गीत में शब्द और मुख्य स्वर जरूर लक्ष्मण मस्तुरिया के हैं, लेकिन भावनाएँ छत्तीसगढ़ महतारी की हैं, जो अपनी धरती की संतानों से कह रही है कि मैं ही महानदी हूँ, मैं ही अरपा और पैरी नदी हूँ। गंगा तो बहुत दूर है, इसलिए पापियों, तुम यहीं तर जाओ।
धरती माता की वंदना का उनका एक खूबसूरत छत्तीसगढ़ी गीत मस्तुरिया की आवाज में काफी लोकप्रिय हुआ था, जिसकी कुछ पंक्तियाँ देखें —
मंय बंदत हौं दिन-रात वो, मोर धरती मईया,
जय होवय तोर, मोर छईयां भुइंया, जय होवय तोर।
राजा-परजा, देवी-देवता तोर कोरा म आइन,
जईसन सेवा करिन तोर, वो तईसन फल ल पाइन।
तोर महिमा कतक बखानौ, ओ मोर धरती मईया,
जय होवय तोर, मोर छईयां भुइंया, जय होवय तोर!
अर्थात — हे धरती माता! मैं दिन-रात तेरी वंदना करता हूँ। हे मुझे शीतल छाया देने वाली भूमि! तेरी जय हो! राजा-प्रजा, देवी-देवता, तेरी गोद में आए और जैसी सेवा की, वैसा ही फल पाया। हे धरती माता! तेरी महिमा का मैं कितना बखान करूं!
अपनी धरती से गहरी आत्मीयता का रिश्ता रखने वाला एक सच्चा कवि ही सच्चे दिल से मन को छू लेने वाली ऐसी पंक्तियों के साथ धरती का जयगान लिख सकता है।
अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी गाँव की सड़क पर या फिर खेतों या जंगलों की पगडंडियों पर, बैलगाड़ी से या नहीं तो सायकल से कहीं जा रहे हों, या आपकी कार किसी सड़क पर कुछ देर के लिए किसी भी कारण से रुक गई हो, चांदनी रात हो और दूर किसी गाँव से लाऊडस्पीकर पर गूंजता यह मीठा-सा नगमा आपके कानों तक पहुँचे, तो मुझे लगता है कि आपको एक अलग ही तरह की अनुभूति होगी —
पता दे जा रे, पता ले जा रे गाड़ी वाला,
तोर नाम के, तोर गाँव के, तोर काम के, पता दे जा।
का तोर गाँव के पार सिवाना, डाक-खाना के नाम का,
थाना-कछेरी के तोरे, पारा-मुहल्ला, जघा का!
शायद नायिका को अपने गाँव से गुजरते गाड़ी वाले से भावनात्मक लगाव हो गया है। तभी तो वह उससे उसके गाँव, डाकघर, थाना-क्षेत्र, कचहरी, पारा-मुहल्ला और जगह का नाम पूछ रही है और मनुहार भी कर रही है कि जाते-जाते वह अपना पता दे जाए और यहाँ का, याने कि नायिका का पता लेता जाए।
इस गीत में प्रेम का एक गहरा दर्शन भी है। कैसे यह इन पंक्तियों में देखें और महसूस करें —
मया नई चिन्हें देसी-बिदेसी,
मया के मोल न तोल,
जात-बिजात न जाने रे मया,
मया मयारू के बोल,
काया माया के सब नाच नचावै,
मया के एक नजरिया।
नायिका कहती है — प्रेम किसी देशी-विदेशी को नहीं पहचानता, प्रेम का कोई मोल-तोल नहीं होता, प्रेम जात-बिजात को भी नहीं जानता, वह सिर्फ मया यानी प्रेम की बोली को ही समझता है।
आज से करीब 50 साल पहले कविता वासनिक की खनकती आवाज में लक्ष्मण के इस गीत का ग्रामोफोन रिकार्ड निकला, तो यह शादी-ब्याह से लेकर हर निजी और सार्वजनिक समारोह में गूंजने लगा। लोग इसे गुनगुनाने के लिए अनायास ही मजबूर हो जाते थे।
माघ-फागुन के रसभीने वासंती मौसम पर उनका यह गीत, उन्हीं की मधुर आवाज में एक अलग ही अंदाज में आज भी लोगों के दिलो-दिमाग पर छा जाता है —
मन डोले रे मांघ फगुनवा,
रस घोले रे मांघ फगुनवा।
राजा बरोबर लगे मौरे आमा,
रानी सही परसा फुलवा,
रस घोले रे मांघ फगुनवा,
मन डोले रे मांघ फगुनवा।
माघ महीने के आखिरी दिनों में फागुन के वासंती कदमों की धीमी-धीमी आहट के बीच आम के मौर की भीनी-भीनी महक और पलाश के पेड़ों पर खिलते सुर्ख लाल फूलों से भला किसका मन नहीं डोलेगा! तभी तो हमारे कवि को यह समय जीवन में रस घोलने का मौसम लगता है। डालियों पर नन्हें-नन्हें फूलों यानी कि मौरों से सजा-धजा आम का पेड़ राजा की तरह और परसा यानी कि पलाश का वृक्ष किसी रानी की तरह लगने लगा है।
यह आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से प्रसारित होने वाले सर्वाधिक लोकप्रिय छत्तीसगढ़ी गीतों में शुमार है। लगभग पैंतीस साल पहले 1975 के आस-पास जब यह रेडियो पर आया, तो हर सुनने वाला सुनता ही रह गया।
लक्ष्मण मस्तुरिया छत्तीसगढ़ के उन गिने-चुने कवियों में से एक थे, जिन्हें नयी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय समारोह के मौके पर लाल किले के मंच से काव्य-पाठ करने का अवसर मिला। लक्ष्मण को यह गौरव आज से 51 वर्ष पहले, 1974 में, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध शायर मुकीम भारती के साथ मिल चुका था। वहाँ 20 जनवरी 1974 को आयोजित काव्य-संध्या में उन्हें गोपालदास नीरज, बालकवि बैरागी, रमानाथ अवस्थी, डॉ. रविन्द्र भ्रमर, इन्द्रजीत सिंह ‘तुलसी’, निर्भय हाथरसी और रामावतार त्यागी जैसे लोकप्रिय कवियों के साथ आमंत्रित किया गया था।
छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक जागरण के ऐतिहासिक रंगमंच ‘चंदैनी गोंदा’ से, आकाशवाणी, दूरदर्शन और कवि-सम्मेलनों के मंच से होते हुए लक्ष्मण मस्तुरिया छत्तीसगढ़ी फिल्मों में भी गीत लिख रहे थे। राज्य-निर्माण के आस-पास बनी ‘मोर छईयां भुइयां’ और उसके कुछ वर्ष बाद आयी ‘मोर संग चलव’ के तो शीर्षक ही लक्ष्मण के दो लोकप्रिय गीतों की सराही गई पंक्तियों पर आधारित हैं।
उन्होंने छत्तीसगढ़ी फिल्म ‘भोला छत्तीसगढ़िया’, ‘पिंजरा के मैना’, ‘पुन्नी के चन्दा’ और ‘मया के बंधना’ में भी मधुर गीत लिखे थे। लक्ष्मण के गीतों को सुरों में सजा कर ग्रामोफोन के जमाने में करीब चालीस एलपी रिकॉर्ड भी बाजार में आए और खूब लोकप्रिय हुए। उनके गीतों पर आधारित सैकड़ों कैसेट्स और ऑडियो व वीडियो एल्बम संगीत के बाजार में हाथों-हाथ लिए जाते रहे हैं।
उनकी प्रकाशित पुस्तकों में 77 छत्तीसगढ़ी कविताओं का संग्रह ‘मोर संग चलव’ (2003), 61 छत्तीसगढ़ी निबंधों का संग्रह ‘माटी कहे कुम्हार से’ (2008) और 71 हिन्दी कविताओं का संकलन ‘सिर्फ सत्य के लिए’ (2008) उल्लेखनीय हैं। इसके पहले छत्तीसगढ़ के महान क्रांतिकारी अमर शहीद वीर नारायण सिंह की जीवन-गाथा पर आधारित उनकी एक लम्बी कविता ‘सोनाखान के आगी’ भी पुस्तक रूप में आ चुकी है।
दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय, भोपाल द्वारा मार्च 2008 में आयोजित अलंकरण समारोह में जिन तीन प्रसिद्ध कवियों को मध्यप्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल श्री बलराम जाखड़ ने सम्मानित किया, उनमें लक्ष्मण मस्तुरिया भी थे, जिन्हें ‘आंचलिक रचनाकार सम्मान’ से नवाजा गया। उनके अलावा प्रसिद्ध शायर निदा फाजली को ‘दुष्यंत अलंकरण’ और साहित्यकार प्रेमशंकर रघुवंशी को ‘सुदीर्घ साधना सम्मान’ से अलंकृत किया गया।
अपने गृह राज्य छत्तीसगढ़ में भी लक्ष्मण को अनेक अवसरों पर अनेक संस्थाओं ने सम्मानित किया है, जिनमें ‘रामचंद्र देशमुख बहुमत सम्मान’ (दुर्ग) और ‘सृजन सम्मान’ (रायपुर) भी शामिल हैं। हमारे समय के वरिष्ठ साहित्यकार, रायगढ़ निवासी डॉ. बलदेव ने लिखा था —
“लक्ष्मण मस्तुरिया के गीत चिर युवा छत्तीसगढ़िया के गीत हैं। अल्हड़ जवानी, उमंग, उत्साह, साहस, आस्था, आशा, विश्वास, स्वाभिमान, उत्कट प्रेम, सर्वस्व समर्पण की भावना, विरह-वेदना और पुनर्मिलन की छटपटाहट की सहजतम अभिव्यक्ति उनके गीतों की विशेषता है। उनके गीतों की लोकप्रियता का रहस्य सिर्फ गले की मिठास और पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक वाद्य-यंत्र नहीं है। ये तो सफलता के महज ऊपरी रहस्य हैं। असली रहस्य है उनके गीतों में कथ्य की नवीनता, रूप-विधान और भाव-सौंदर्य।”
डॉ. बलदेव भी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन इन शब्दों में उनकी भावनाएँ लक्ष्मण मस्तुरिया की रचनाओं की विशेषता को प्रकट करती हैं।
साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में लक्ष्मण मस्तुरिया का अतुलनीय योगदान था। उस दिन उनके निधन की खबर से प्रदेश की साहित्यिक-सांस्कृतिक बिरादरी सहित उन्हें चाहने वाले लाखों लोग स्तब्ध रह गए।
छत्तीसगढ़ के लोग चाहते थे कि अपनी माटी का जयगान करने वाले लक्ष्मण, सृजन और श्रृंगार गीतों से मानव-मन में जीवन का आनंद-रस घोलने वाले लक्ष्मण बरसों-बरस इसी तरह लिखते रहें और वे मधुर आवाज में इस धरती की महिमा का गुणगान करते रहें, लेकिन अफसोस कि नियति ने ऐसा नहीं होने दिया।