जनजातीय संस्कृति और स्वत्व के प्रहरी कार्तिक उरांव
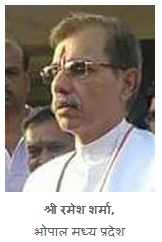 यह भारत की आज़ादी का वह दौर था, जब विदेशी सत्ता से मुक्ति का संघर्ष तो पूरा हो चुका था, लेकिन भारत की आत्मा, उसकी संस्कृति, परंपरा और स्वत्व की पुनर्स्थापना का संघर्ष अभी भी जारी था। स्वतंत्रता ने भले ही हमें राजनीतिक आज़ादी दी हो, पर मानसिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अभियान कई महापुरुषों ने अपने जीवन से आगे बढ़ाया। इन्हीं में एक नाम है वनवासी नायक, विचारक और समाज सुधारक कार्तिक उरांव का।
यह भारत की आज़ादी का वह दौर था, जब विदेशी सत्ता से मुक्ति का संघर्ष तो पूरा हो चुका था, लेकिन भारत की आत्मा, उसकी संस्कृति, परंपरा और स्वत्व की पुनर्स्थापना का संघर्ष अभी भी जारी था। स्वतंत्रता ने भले ही हमें राजनीतिक आज़ादी दी हो, पर मानसिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अभियान कई महापुरुषों ने अपने जीवन से आगे बढ़ाया। इन्हीं में एक नाम है वनवासी नायक, विचारक और समाज सुधारक कार्तिक उरांव का।
वे उन विभूतियों में से थे, जिन्होंने न केवल आदिवासी समाज में सांस्कृतिक जागरण का दीप जलाया, बल्कि धर्मांतरण कर लेने वालों को आरक्षण का लाभ न देने के अभियान को भी एक राष्ट्रीय विमर्श का विषय बनाया। पर दुर्भाग्य यह रहा कि जितनी गहराई उनके चिंतन में थी, उतनी व्यापकता उनके नाम की चर्चा में नहीं दिखाई देती।
भारत के वनक्षेत्रों में दो प्रकार के संघर्ष हमेशा रहे — एक राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा के लिए, और दूसरा संस्कृति की रक्षा के लिए। जहाँ सीमाओं पर वीर सिपाही लड़े, वहीं गांव-गांव में आदिवासी समाज अपनी पहचान और परंपरा की रक्षा में डटा रहा। अंग्रेजों के शासनकाल में मिशनरी संस्थाओं ने जब वनवासी जीवन और संस्कृति को तोड़ने का प्रयास शुरू किया, तब इस सांस्कृतिक संघर्ष की जड़ें और गहरी हो गईं।
सन् 1773 के आसपास मिशनरियों ने भारत के जंगल इलाकों में अपने पैर पसारने शुरू किए, और पचास वर्षों के भीतर वे देशभर के अधिकांश आदिवासी क्षेत्रों तक पहुँच गए। धर्मांतरण के इस दौर में, जब आदिवासी अपनी जड़ों से कटते जा रहे थे, तभी 29 अक्टूबर 1924 को झारखंड के गुमला ज़िले के करौंदा लिटाटोली गांव में कार्तिक उरांव का जन्म हुआ। वे ‘कुरुख’ जनजाति से थे। उनके पिता जयरा उरांव समाज में सम्मानित व्यक्ति थे और माता बिरसी उरांव परंपराओं की गहरी संवाहिका थीं।
कार्तिक चार भाइयों में सबसे छोटे थे। कार्तिक माह में जन्म लेने के कारण उनका नाम भी ‘कार्तिक’ रखा गया, एक ऐसा नाम जो आगे चलकर आदिवासी स्वाभिमान का प्रतीक बन गया।
प्रारंभिक शिक्षा गाँव में ही पूरी करने के बाद 1942 में उन्होंने गुमला से हाई स्कूल पास किया और आगे की पढ़ाई के लिए पटना पहुँचे। यह वही समय था जब गांधीजी के आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन की लहर पूरे देश में थी। कार्तिक उरांव न केवल इन प्रभात फेरियों में शामिल होते, बल्कि अपने साथियों को भी देशभक्ति के लिए प्रेरित करते।
उन्होंने पटना साइंस कॉलेज से इंटरमीडिएट और बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। पर उनका ज्ञान-पिपासु मन वहीं नहीं रुका, उन्होंने इंजीनियरिंग की विभिन्न शाखाओं में अध्ययन जारी रखा और कुल नौ डिग्रियाँ अर्जित कीं। बाद में वे अमेरिका और लंदन भी गए, जहाँ से उन्होंने इंजीनियरिंग के साथ-साथ वकालत की डिग्री भी प्राप्त की। वे भारत के पहले ऐसे व्यक्ति बने, जिन्होंने इंजीनियरिंग में नौ डिग्रियाँ और कानून की डिग्री एक साथ प्राप्त की।
लंदन में रहते हुए उन्होंने हिंकले पॉइंट एटॉमिक पावर स्टेशन का डिज़ाइन तैयार किया, जो उस समय विश्व का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र था। इस उपलब्धि ने उन्हें वैश्विक पहचान दिलाई। पर उनके भीतर का भारतीय कभी पश्चिम में बस नहीं सका। पंडित नेहरू के आग्रह पर वे भारत लौट आए और हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन में प्रमुख पद संभाला।
नौकरी करते हुए भी उनका मन समाज सेवा की ओर खिंचता रहा। उन्होंने अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना की, एक ऐसा संगठन जो राजनीति से परे रहकर आदिवासी समाज के सांस्कृतिक उत्थान के लिए समर्पित था।
बाद में नेहरूजी के अनुरोध पर वे राजनीति में आए। 1962 में उन्होंने लोहरदगा से लोकसभा चुनाव लड़ा , पहली बार हार मिली, लेकिन 1967 में वे वहीं से संसद पहुँचे। संसद में उनका प्रवेश एक मिशन की तरह था, न कि सत्ता की सीढ़ी के रूप में।
कार्तिक उरांव का उद्देश्य स्पष्ट था। उन्होंने पूरे देश में घूम-घूमकर तीन सूत्रीय अभियान चलाया –
-
आदिवासी समाज अपनी सांस्कृतिक परंपराओं और रीति-रिवाजों को जिए और संरक्षित रखे।
-
सभी आदिवासी समाज हिंदू संस्कृति का अंग हैं।
-
धर्मांतरण करने वालों को अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण और सुविधाओं से वंचित रखा जाए।
वे अपने तर्क लोकजीवन के उदाहरणों से सिद्ध करते थे। कहते थे कि निषादराज गुह, माता शबरी, कण्णप्पा जैसे चरित्र इसी समाज से निकले हैं यह प्रमाण है कि आदिवासी समाज प्राचीन भारत का अभिन्न अंग है। वे गीतों और लोककथाओं से उदाहरण देते कि कैसे आदिवासी गीतों में कृष्ण, राम और सीता का स्मरण मिलता है। इसीलिए वे कहते थे “हमारा समाज कभी अलग नहीं था, केवल भुला दिया गया है।”
उनकी वाणी में ऐसा तेज था कि लोग उन्हें ‘पंखराज साहेब’ और ‘काला हीरा’ कहकर पुकारते। संसद में जब वे बोलते, तो शांति छा जाती। एक अंग्रेज़ी अख़बार The Hindu ने उन्हें लिखा “The Tiger Who Roars in Parliament.”
कार्तिक उरांव का सबसे बड़ा संघर्ष धर्मांतरण और आरक्षण के दुरुपयोग को लेकर था। उनका कहना था “जो व्यक्ति अपनी आस्था बदल चुका है, उसे उन सुविधाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए जो एक परंपरागत आदिवासी को अपने सामाजिक पिछड़ेपन के कारण दी गई हैं।”
उन्होंने संसद में 1967 में अनुसूचित जाति/जनजाति आदेश संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। समिति बनी, सिफारिशें भी आईं, स्पष्ट कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाता है, तो वह अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। परंतु जब यह विधेयक चर्चा के लिए आया, तो मिशनरियों के दबाव और राजनीतिक कारणों से इसे टाल दिया गया।
कार्तिक उरांव ने 322 लोकसभा और 26 राज्यसभा सदस्यों के हस्ताक्षरों के साथ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा था – “सांस्कृतिक अस्तित्व की रक्षा, राजनीतिक हितों से कहीं बड़ी बात है।” पर यह संशोधन विधेयक संसद भंग होने के साथ इतिहास के पन्नों में सिमट गया।
यह असफलता उनके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा बनी रही। उन्होंने बाद में “बीस वर्ष की काली रात” नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने मिशनरियों की रणनीतियों और आदिवासियों की सरलता का विश्लेषण किया। उन्होंने लिखा —
“अंग्रेजों के 150 वर्षों में जितना धर्मांतरण नहीं हुआ, उतना स्वतंत्र भारत में हो गया।”
उनकी स्पष्टवादिता और संघर्षशीलता ने उन्हें आदिवासी समाज का सच्चा प्रहरी बना दिया। 8 दिसंबर 1981 को, संसद भवन में ही, दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उस समय वे भारत सरकार में उड्डयन और संचार मंत्री थे।
उनके बाद उनकी पत्नी सुमति उरांव और पुत्री गीताश्री उरांव ने भी राजनीति में कदम रखा, पर कार्तिक उरांव का वह सांस्कृतिक अभियान, वह वैचारिक चेतना – वैसी गति फिर कभी न पा सकी।
कार्तिक उरांव का जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि उस संघर्ष की गाथा है जिसमें भारत का आदिवासी समाज अपनी पहचान और आत्मगौरव की रक्षा करता रहा। वे मानते थे – “विकास की पहली शर्त अपनी जड़ों से जुड़े रहना है।” उनकी जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि स्वतंत्रता केवल राजनैतिक नहीं, सांस्कृतिक और आत्मिक भी होती है, और इस स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कुछ लोग सचमुच अपना जीवन समर्पित कर देते हैं।




