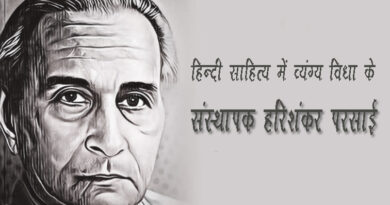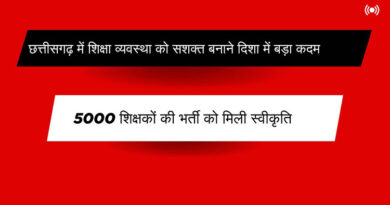सीमाओं से परे बहती हिन्दी भाषा की धारा : हिन्दी दिवस विशेष

हमारी पीढी जब स्कूल पहुंची तो पाठ्यक्रम हिन्दी में ही था। मातृ भाषा से हम स्कूल में हिन्दी की ओर बढने लगे क्योंकि मातृ भाषा की गिनती बोलियों में थी। आजादी के बाद हमारा क्षेत्र भी हिन्दी पट्टी में सम्मिलित था। इस तरह पांचवी तक सारी शिक्षा हिन्दी में ही हुई, इसके बाद छठवीं से अंग्रेजी वर्णमाला पाठ्यक्रम में सम्मिलित हुई। आगे की पढाई भी हिन्दी माध्यम में हुई। तब हिन्दी के उद्भव एवं विकास के विषय में अधिक जानकारी नहीं थी और न ही इतना जानने के लिए बुद्धि लगाने की आवश्यकता थी।
कक्षा आठवी में मेरे हाथों में स्वामी दयानंद कृत सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ आया। इस ग्रंथ का पहला संस्करण 1875 ईस्वीं में प्रकाशित हुआ। इसकी प्रस्तावना में भी बताया गया था कि तत्कालीन समय में हिन्दी के भविष्य को देखते हुए स्वामी जी ने इस ग्रंथ को हिन्दी में लिखा। यह उनकी दूरगामी सोच का ही परिणाम था। जो आज भी हिन्दी का प्रभाव क्षेत्र बढने के कारण पढा जा रहा है और लोग उससे प्रेरित हो रहे हैं।
दूसरी घटना तब घटी जब नवमी की कक्षा में स्कूल की लायब्रेरी में एक किताब मिली, जिसका नाम चंद्रकांता था। यहीं से हिन्दी के विषय में जानकारी मिली। एक स्थान पर पढा कि बाबू देवकीनंदन खत्री के द्वारा लिखित यह उपन्यास इतना अधिक चर्चित हुआ कि लाखों लोगों ने इसे पढने के लिए हिन्दी सीखी। कहते हैं यह उपन्यास इतना लोकप्रिय हुआ कि गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों, जैसे दक्षिण भारत, अंग्रेज अधिकारी और अन्य विद्वान भी हिंदी सीखने को प्रेरित हुए। सटीक संख्या के बजाय, ऐतिहासिक स्रोतों में इसे “लाखों” के रूप में वर्णित किया गया है, जो उस युग की हिंदी के प्रसार में मील का पत्थर साबित हुआ।
इन दोनों घटनाओं से ये साबित हुआ कि वर्तमान हिन्दी के बजाय तत्कालीन समय में अन्य कोई भाषा, लेखन एवं राजकाज की भाषा थी। इसलिए बाद में लोगों को हिन्दी सीखनी पड़ी। आज गंगा जी में बहुत पानी बह गया है। हिन्दी राजकाज के साथ आमजन की भाषा भी बन रही है। धीरे धीरे इसका प्रभाव क्षेत्र बढ रहा है और हिन्दी के ग्रंथों के साथ उनके रचनाकार भी विश्व में अपना स्थान बना रहे हैं तथा विश्व में हिन्दी स्थापित होते जा रही है। भारत के कई प्रांतों में यह सम्पर्क भाषा के रुप में कार्य कर रही है। हिन्दी को वैश्विक स्त्तर तक स्थापित करने में फ़िल्मों का बड़ा योगदान है।
लगता है कि आज हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, यह दिलों को जोड़ने वाली डोर है। यह गीतों की मधुर लय में बहती है, कहानियों में जीवन्त हो उठती है और हमारी भावनाओं को शब्द देती है। विश्व में जहाँ कहीं भी जब हिंदी की बात होती है, सामने भारत की ही छवि दिखाई देती है। यहां करोड़ों लोग इसे अपनी जुबान और पहचान मानते हैं। लेकिन हिंदी की धारा भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रही। यह सीमाओं को लांघकर दुनिया के कोने-कोने में पहुँच गई है। आज यह वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जिसके करीब 60 करोड़ से अधिक बोलने वाले हैं। यह केवल एक आँकड़ा नहीं, बल्कि भारतीय प्रवास, संघर्ष और सांस्कृतिक धरोहर की जीवित कहानी है।
हिंदी की जड़ें इंडो-आर्यन भाषा परिवार से जुड़ी हैं और यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भारत में यह न केवल साहित्य, प्रशासन और शिक्षा में बल्कि सिनेमा और मीडिया के माध्यम से भी गहराई से जुड़ी है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान लाखों भारतीय मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर के रूप में दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में भेजा गया। वे अपने साथ हिंदी की बोली, गीत और परंपराएँ लेकर गए। यही वजह है कि आज एशिया से लेकर कैरिबियन और अफ्रीका से लेकर यूरोप-अमेरिका तक हिंदी की गूंज सुनाई देती है।
नेपाल में लगभग 80 लाख लोग हिंदी बोलते हैं। यह भाषा वहाँ भारत और नेपाल के सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने का काम करती है। खासकर तराई क्षेत्र में हिंदी रोज़मर्रा की भाषा है। बॉलीवुड फिल्में, हिंदी गाने और धार्मिक भजन यहाँ बेहद लोकप्रिय हैं। नेपाली भाषा के वर्चस्व के बावजूद हिंदी समुदायों को भारत से जोड़ने वाली कड़ी बनी हुई है।
फिजी में लगभग 3.8 लाख लोग ‘फिजी हिंदी’ बोलते हैं, जो भोजपुरी, अवधी और अंग्रेज़ी का मिश्रण है। गन्ने के खेतों में काम करने आए भारतीय मजदूरों के वंशज आज इसे अपनी सांस्कृतिक पहचान मानते हैं। यहाँ होली, दिवाली जैसे त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं और हिंदी धार्मिक ग्रंथों की कथाओं के माध्यम से पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ रही है।
मॉरीशस में करीब साढ़े चार लाख लोग हिंदी बोलते हैं। यहाँ हिंदी न केवल स्कूलों में पढ़ाई जाती है बल्कि राजनीति और मीडिया में भी प्रचलित है। मॉरीशस को अक्सर “छोटा भारत” कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भारतीय संस्कृति और हिंदी का गहरा असर दिखाई देता है।
सूरीनाम, गयाना और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में भी हिंदी के स्वर गूंजते हैं। यहाँ ‘सारनामी हिंदी’ और ‘कैरिबियन हिंदुस्तानी’ बोली जाती है। स्थानीय संस्कृति के साथ घुलमिलकर हिंदी ने यहाँ एक नया रूप ले लिया है। हालांकि, नई पीढ़ी में अंग्रेज़ी का प्रभाव बढ़ने से हिंदी के संरक्षण की चुनौती भी सामने है।
संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 8.6 लाख लोग हिंदी बोलते हैं। न्यू जर्सी, टेक्सास और कैलिफोर्निया जैसे राज्यों में भारतीय समुदाय मजबूत है। यहाँ हिंदी स्कूल और सांस्कृतिक संगठन सक्रिय हैं। न्यूयॉर्क की सड़कों पर हिंदी बातचीत सुनाई देना या सिलिकॉन वैली में हिंदी में मजाक साझा करना अब असामान्य नहीं है।
यूनाइटेड किंगडम में करीब 5 लाख हिंदी भाषी हैं। लंदन का साउथॉल इलाका “लिटिल इंडिया” कहलाता है, जहाँ दुकानों और रेस्टोरेंट्स में हिंदी के बोर्ड दिखते हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएई में भी बड़ी संख्या में हिंदी बोलने वाले समुदाय बसे हैं। खासकर खाड़ी देशों में, जहाँ लाखों भारतीय काम करते हैं, हिंदी एक साझा भाषा की तरह लोगों को जोड़ती है।
दक्षिण अफ्रीका में 2.5 लाख हिंदी भाषी हैं। डरबन जैसे शहरों में भारतीय संस्कृति अब भी जीवित है। यही वह धरती है, जहाँ गांधीजी ने अपने आंदोलन की शुरुआत की थी। सिंगापुर, बांग्लादेश और मलेशिया में भी हिंदी को समझा और अपनाया जाता है।
हिन्दी को विश्व के बड़े मंचों तक पहुंचाने में हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का भी योगदान वृहद रहा है इससे वैश्विक स्तर पर हिंदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषण दिए जा रहे हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने इसे नई ऊर्जा दी है। लेकिन चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। प्रवासी समुदायों में नई पीढ़ी अंग्रेज़ी या स्थानीय भाषा को प्राथमिकता देती है, जिससे हिंदी को संरक्षित रखने की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है।
हिंदी आज केवल भारत की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की भाषा बन चुकी है। यह उन प्रवासियों की स्मृति है, जिन्होंने अपनी संस्कृति और भाषा को हजारों मील दूर जाकर भी जीवित रखा। हिंदी का यह वैश्विक स्वरूप हमें याद दिलाता है कि भाषा केवल संवाद का साधन नहीं, बल्कि पहचान, एकता और भावनाओं की अभिव्यक्ति है। जैसे कोई पुराना गीत दूर-दूर तक गूंजता है, वैसे ही हिंदी भी दुनिया भर में अपनी मधुरता से दिलों को जोड़ती रहेगी।