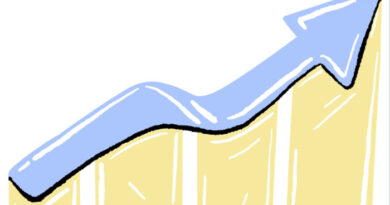पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन : भारतीय जीवन का समग्र दृष्टिकोण
 विश्व की आधुनिक शासन प्रणालियों में बहुत से सिद्धांत सामने आए। इन सिद्धांतों को सूत्र रूप प्रस्तुत करने के लिए कुछ शब्द भी आए, जैसे साम्यवाद, पूँजीवाद, समाजवाद आदि। दीनदयाल जी ने इन सबको अपूर्ण और अव्यवहारिक बताया और एकात्म मानव दर्शन प्रस्तुत किया, जिसका आधार चतुर्पुरुषार्थ है।
विश्व की आधुनिक शासन प्रणालियों में बहुत से सिद्धांत सामने आए। इन सिद्धांतों को सूत्र रूप प्रस्तुत करने के लिए कुछ शब्द भी आए, जैसे साम्यवाद, पूँजीवाद, समाजवाद आदि। दीनदयाल जी ने इन सबको अपूर्ण और अव्यवहारिक बताया और एकात्म मानव दर्शन प्रस्तुत किया, जिसका आधार चतुर्पुरुषार्थ है।
सबसे पहले तो दीनदयाल जी शब्द “वाद” के समर्थक नहीं थे। उनका कहना था कि यदि वाद होगा तो इसका प्रतिवाद भी होगा और प्रतिवाद होगा तो विवाद होगा। जीवन के विकास का सिद्धांत विवाद और प्रतिवाद रहित होना चाहिए, क्योंकि विवाद और प्रतिवाद में अनावश्यक ऊर्जा और समय नष्ट होता है तथा नकारात्मकता उत्पन्न होती है। भविष्य की विकास यात्रा विवाद रहित होनी चाहिए।
उनका कहना था कि प्रकृति विविधता से भरी है। विविधता ही प्रकृति का सौन्दर्य है, तब इसे एक स्वरूप कैसे माना जा सकता है? एक आदर्श व्यवस्था वह है जो प्रत्येक प्राणी या जीवन को उसके मौलिक स्वरूप और गुण-कर्म के आधार पर विकास का अवसर दे। यदि एक व्यक्ति पुरुषार्थ कर रहा है और दूसरा व्यक्ति अकर्मण्य है, तब दोनों में साम्य कैसे होगा?
दूसरा, यदि पूँजी को प्रधानता दी तो अनाचार बढ़ेगा। व्यक्ति को मार्ग या कुमार्ग का कोई भान नहीं होगा और वह केवल पूँजी के पीछे भागेगा। तीसरा, समस्त मानवों का महत्व तो समान हो सकता है, पर समाज तो समूह से बनता है और समूह के मूल में क्षेत्रीयता और गुण-धर्म होता है। अतः हमें साम्यवाद, पूँजीवाद, समाजवाद या मानववाद की बात करने की बजाय मानव दर्शन की बात करनी चाहिए। और इसका आधार चार पुरुषार्थ होना चाहिए।
चतुर्पुरुषार्थ का आधार
दीनदयाल जी ने भारतीय वाङ्मय का गहराई से अध्ययन किया था। चतुर्पुरुषार्थ का सिद्धांत वेदों, उपनिषदों और पुराणों में वर्णित है, जिसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के रूप में विभाजित किया गया है।
उन्होंने धर्म को उसके व्यापक संदर्भ में परिभाषित किया। पूजा-उपासना पद्धति धर्म का एक भाग अवश्य है, पर वही संपूर्ण नहीं। धारणीय कर्तव्य को धर्म कहा गया है। जैसे शिक्षक का धर्म पढ़ाना है।
ठीक उसी प्रकार मोक्ष को वे लक्ष्य की परम स्थिति मानते थे। जिस प्रकार आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य परम मुक्ति है, उसी प्रकार हमारे कर्म-कर्त्तव्य की भी परम स्थिति हमारा लक्ष्य प्राप्त करना है। इस प्रकार उन्होंने व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए इन चार पुरुषार्थ के आधार पर एक जीवन दर्शन दिया, जिसे एकात्म मानव दर्शन माना गया।
यह एकात्म मानव दर्शन पहली बार 1964 में जनसंघ के ग्वालियर अधिवेशन में रखा गया और अगले विजयवाड़ा अधिवेशन में सर्वसम्मत स्वीकार कर लिया गया। दीनदयाल जी ने 22 से 25 अप्रैल 1965 में चार दिन लगातार इस दर्शन पर आधारित व्याख्यान दिया, जिसमें आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वरूप का प्रस्तुतिकरण था।
एकात्म मानववाद : अखंड दृष्टि
एकात्म मानववाद एक ऐसी अवधारणा है जो समूची सृष्टि के जीवन को अभिव्यक्त करती है। इसके केंद्र में व्यक्ति, व्यक्ति से जुड़ा घेरा परिवार के रूप में, परिवार से जुड़ा हुआ घेरा समाज के रूप में, समाज और समाजों का विस्तार राष्ट्र के रूप में, राष्ट्र का विस्तार विश्वरूप और फिर अनंत ब्रह्माण्ड।
इस अखण्ड ब्रह्माण्ड आकृति में एक का अस्तित्व दूसरे पर निर्भर है। सब परस्पर सहअस्तित्व हैं, एक-दूसरे के पूरक और सहयोगी हैं। तब कैसे कोई एक पक्ष दूसरे को छोड़कर अपना विस्तार कर सकता है?
दीनदयाल जी ने पश्चिमी और अन्य विदेशी अवधारणाओं के आधार पर भारत के विकास भविष्य की कल्पना करने वालों से आग्रह किया कि जब भारत ने विदेशी और पाश्चात्य साम्राज्य को नकार दिया, तब हमें उनकी नीतियाँ और दर्शन भी नकार देने चाहिए।
उन्होंने इस मानसिकता से उबरने का आह्वान किया कि “हमें कुछ संशोधनों के साथ इन पाश्चात्य शैली को ही स्वीकारना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोई अपना चिंतन नहीं, कोई मार्ग नहीं है। हम तो राष्ट्र थे ही नहीं। पाश्चात्यों ने ही आकर हमको राष्ट्र बनने के लिए तैयार किया है।”
दीनदयाल जी ने दृढ़ता से कहा कि भारत तो उस समय भी एक राष्ट्र रहा है जब विश्व की संस्कृतियों का अंकुरण भी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि हमारी राष्ट्र-राज्य परिकल्पना ‘सांस्कृतिक राष्ट्रभाव’ की है। हमारी एक गौरवसम्पन्न राष्ट्र-परंपरा है, जिसके केन्द्र में ज्ञान है। हमें इसी ज्ञान-परम्परा में भारत का भविष्य खोजना चाहिए।
विदेशी विचारधाराओं की आलोचना
उन्होंने कहा कि विदेशी जगत की प्राथमिकता में मानव नहीं है, केवल विजय है और आर्थिक समृद्धि का चिंतन है, जो मानवीय अधिकार और मान दोनों के लिये घातक है। इसीलिए पश्चिम का अभियान कोई भी हो—धार्मिक, आर्थिक या राजनीतिक—सबमें टकराहट है। सब मनुष्य को अपना दास बनाना चाहते हैं। जबकि भारत मानवीय सम्मान को महत्व देता है।
दीनदयाल जी ने एक ओर जहाँ पश्चिमी चिंतन को अधूरा बताया, वहीं पश्चिम की इस बहस को सार्थक बताया जिसमें पहली बार मानवाधिकार विषय आया। उन्होंने कहा कि यह एक मानवीय चर्चा है, हमें भी जानना चाहिए और कुछ सीखना भी चाहिए। लेकिन यदि इसमें कोई द्वंद्वमूलक निष्कर्ष आता है तो हमें उसका अनुपालन नहीं करना चाहिए।
सृष्टि और मानव की एकात्मता
दीनदयाल जी ने कहा कि हमें भविष्य के विकास की परिकल्पना मानव से मानव तक ही नहीं, अपितु मानव से इस मंडलाकार सृष्टि के एकात्म स्वरूप को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ना होगा।
भारत में इसी चिंतन यात्रा को धर्म कहा गया है—‘यतोऽभ्युदय निःश्रेयस संसिद्धि स धर्म।’ अर्थात् यह व्यष्टि, समिष्टि, सृष्टि व परमेष्ठी की एकात्मता का विचार है।
यह विचार सभी दृश्यमान जगत में एकात्मता खोजता है। उन्होंने समझाया कि संसार में पृथक दिख रहा है, वह पृथक नहीं है। यह तो स्वरूप की विविधता है। जो ‘पिंड’ में है वही ‘ब्रह्माण्ड’ में है। अर्थात मानव की देह में जो तत्व या पदार्थ हैं, वे ही सब ब्रह्माण्ड में हैं।
आज मानव अपने को पृथक मानकर दूसरे मानव से युद्ध कर रहा है। परिवार, जाति, वंश, पंचायत सबको अपना दुश्मन मान रहा है। यह मानवता के लिए घातक है। उन्होंने चेतावनी दी कि साम्यवाद के नाम पर जो मार्ग खोजा गया है, यह तानाशाही की ओर जा रहा है। विकास के नाम पर प्रकृति से युद्ध कर रहा है, जो भविष्य में विनाश की भयानक विभीषिका को आमंत्रण है।
भारतीय चिंतन : अधिकार नहीं, सेवा भाव
उन्होंने कहा कि अध्यात्म को अनदेखा नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा हुआ तो मन स्वेच्छाचारी होगा और इन्द्रियाँ भोग के लिए लालायित। इससे दुख के अतिरिक्त कुछ न मिलेगा।
भारतीय चिंतन अधिकार-भाव का नहीं, सेवा-भाव का है, संबंध-भाव का है। तभी तो सबसे रिश्ते जोड़े जाते हैं—धरती ‘माता’ है, चन्द्रमा ‘मामा’ है, पर्वत ‘देवता’ हैं, नदियाँ ‘माता’ हैं, बंदर ‘मामा’ हैं। चींटी से लेकर हाथी तक सभी परस्पर जुड़े हुए हैं। संसार में दूसरा नहीं, कोई पराया नहीं। सब एक-दूसरे के पूरक हैं। पूरी धरती और धरती के समस्त निवासी एक कुटुम्ब हैं।
मानव और सृष्टि की समग्रता
एकात्मता में ही समग्रता है। समग्रता के अभाव में नकारात्मकता आती है, तनाव आता है, मानवता आक्रांत होती है। ब्रह्माण्ड की समग्रता की भाँति ही व्यक्ति की भी समग्रता होती है। सुख, संतोष और आनंद के लिये इस समग्रता का चिंतन करना होगा।
जिस प्रकार व्यक्ति का अस्तित्व केवल शरीर नहीं होता—मन, बुद्धि और आत्मा होती है। शरीर में अंग-प्रत्यंग होते हैं, इनमें से एक की हानि व्यक्ति को विकलांग बना देती है। उसी प्रकार सृष्टि के विराट स्वरूप की पूर्णता ही मानव अस्तित्व की पूर्णता है। सुख की पृथकता से व्यक्ति सुखी नहीं होता, उसे एकात्म सुख चाहिए। वही प्रसन्नता का आधार और आनंद का मार्ग भी है।
राज्य और समाज की भूमिका
दीनदयाल जी ने कहा कि सरकार को केवल सत्ता संचालन का यंत्र नहीं कहा जा सकता। वह समाज भी है, उसे संस्कृति से पृथक नहीं माना जा सकता।
उसी प्रकार सृष्टि के पंच-महाभूत—”पृथ्वी, जल, आकाश, प्रकाश और वायु”—को शुद्ध और सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ना है, तभी मानव सुखी होगा। उन्होंने कहा कि समष्टि, सृष्टि तथा परमेष्ठी से एकात्म हुआ मानव ही विराट पुरुष है। जो ‘धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष’ के रूप में चतुर्पुरुषार्थ कहलाते हैं, इनकी सम्पूर्ति ही एक आदर्श समाज और राष्ट्र व्यवस्था का रूप होगा।