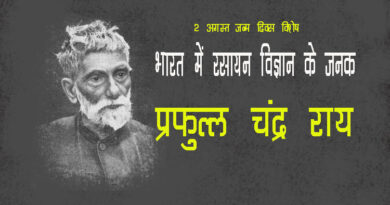वैदिक युग से आधुनिक काल तक सोलह श्रृंगार की सांस्कृतिक यात्रा

वैदिक युग से ही स्त्री को ईश्वर(प्रकृति) की मनोहर रचनाओं में से एक माना जाता रहा है। वराहमिहिर के अनुसार, ईश्वर ने स्त्री के अतिरिक्त कोई अन्य आभूषण कभी नहीं रचा है—जिसका स्पर्श, ध्वनि, दृष्टि या विचार भी मनुष्य के लिए अपार आनंद का स्रोत है (बृहत्संहिता 74/4)। वाल्मीकि ने सुन्दर स्त्री के शारीरिक लक्षणों को उपयुक्त विशेषणों से वर्णित किया है (वाल्मीकि रामायण 3/46, 5/15, 6/12)। कालिदास नारी (नायिका) के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि स्त्री आभूषणों का आभूषण है (विक्रमोर्वशीयम् 2/3)।
सनातनी स्त्रियों को रंग-बिरंगे वस्त्रों, आभूषणों, फूलों, इत्र, क्रीम और सौंदर्य प्रसाधनों से स्वयं को सजाने का सदा से ही बहुत इच्छा रहा है। इस श्रृंगार के पीछे सामान्य उद्देश्य आकर्षक दिखना होता है, और विशिष्ट इसमें जोड़ा गया उद्देश्य अपने जीवनसाथी प्रकृति केन्द्रित होकर एक दूसरे को परस्पर प्रसन्न करना और मनोवैज्ञानिक रूप से तथा सभी दृष्टिकोण से स्वस्थ रखना है। संस्कृत शब्द श्रृगार का तात्पर्य प्रेम की भावना, श्रृंगार रस से है, जो आसक्ति (रति) की भावना से उत्पन्न होता है।
शरीर की सजावट की कला के लिए प्राचीन साहित्य में कई तकनीकी शब्द मिलते हैं। वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र (7/1/59/3) में इसे शुभंकरनाम कहा है। अमरकोश (2/6/100) में हमें इस कला को दर्शाने के लिए कई शब्द मिलते हैं, जैसे परिकर्म, मण्डन, प्रसादन, भूषण, अलंकार, अकल्प, परिस्कर्ण। भरत और रुय्यक ने अलंकार शब्द को स्वीकार किया है, जबकि कालिदास ने इस कला के लिए प्रसादन का प्रयोग किया है।
पहली बार, हमें पाली ग्रंथ ब्रह्मजालसुत्त में बीस प्रकार के शरीर अलंकरणों का उल्लेख मिलता है। ये हैं:
1. इत्र लगाना, 2. मलना, 3. अंगों को दबाना, 4. स्नान करना, 5. माला पहनना, 6. कंगन, 7. आभूषण, 8. चेहरे पर पाउडर लगाना, 9. चेहरे का श्रृंगार, 10. छड़ी पकड़ना, 11. छोटे पंखे, 12. छाता, 13. नालिका (कमल का डंठल), 14. तलवार, 15. जूते पहनना, 16. आंखों में काजल लगाना, 17. बालों की कलगी बांधना, 18. सिर पर पगड़ी, 19. दर्पण पकड़ना, 20. सोने और चांदी के धागों के वस्त्र पहनना।
आयुर्वेद के प्राचीन विद्वान सुश्रुत ने दाँतों को साफ़ करने, शरीर पर तेल मलने, पान चबाने और शारीरिक व्यायाम करने को चार कलाओं में शामिल किया है। इनमें से कई अलंकरण अभ्यास के रूप में थे, जिससे उनकी संख्या बीस हो गई। ये अलंकरण सामान्य थे और इन्हें केवल महिलाओं के लिए विशिष्ट अलंकरण कलाओं के रूप में नहीं माना जाता था। बाद के काल में श्रृंगारों की संख्या को केवल सोलह तक सीमित करने की एक लोकप्रिय परंपरा शुरू हुई, जिसे षोडश (सोलह) श्रृंगार कहा जाता था।
प्राचीन हिंदू पूजा पद्धति में देवताओं के सम्मान में सोलह अनुष्ठान शामिल हैं, जिन्हें षोडशोपाचार कहा जाता है। कहा जाता है कि चंद्रमा के सोलह अंक या भाग होते हैं, जिन्हें कलाएँ कहा जाता है। वैदिक परंपरा में प्रजापति को षोडशी प्रजापति कहा जाता था/है। इसी प्रकार, श्रीकृष्ण को भी पूर्ण–पुरुषोत्तम माना जाता है, जिनकी सोलह कलाएँ (चिह्न) हैं। सोलह वर्ष की युवती (षोडशी) को सौंदर्य की मूर्ति माना जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन परंपराओं ने सौंदर्यशास्त्रियों को विभिन्न श्रृंगारों की सीमा में सीमित करने के लिए प्रभावित किया होगा और इस प्रकार सोलह श्रृंगारों की अवधारणा बनी।
श्रृंगार-क्रम धीरे-धीरे लोकप्रिय होते गए। सोलह श्रृंगारों का पहला उल्लेख वल्लभदेव (15वीं शताब्दी) द्वारा रचित शुभाशितावली नामक श्लोक में मिलता है। ये सोलह श्रृंगार हैं:
1. स्नान, 2. साड़ी पहनना, 3. गले में माला डालना, 4. माथे पर तिलक लगाना, 5. आँखों में काजल लगाना, 6. कुंडल (कान की बाली), 7. नाक में नथनी, 8. बालों को सजाना या चोटी बनाना, 9. कंचुक (ब्लाउज) पहनना, 10. पायल पहनना, 11. इत्र लगाना, 12. कंगन पहनना, 13. लाल लाख से पैर रंगना, 14. कमर में करधनी पहनना, 15. पान चबाना, 16. दर्पण पकड़ना।
चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूपगोस्वामी (1533 ई.) ने उज्ज्वलनीलमणि में राधा के सोलह श्रृंगारों का वर्णन करते हुए वल्लभदेव द्वारा दी गई सूची में कुछ परिवर्तन किए हैं।
सोलह श्रृंगारों की अवधारणा का उल्लेख प्रारंभिक हिंदी साहित्य में भी मिलता है। कबीर ने सोलह के लिए नवसठ शब्द का प्रयोग किया है और गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में ऐसा ही किया है।
इस प्रकार सोलह श्रृगारों की परंपरा मध्यकालीन मुगल काल के दौरान दृढ़ता से स्थापित हुई, हालांकि इसमें कुछ परिवर्तन और नई चीजें जोड़ी गईं।