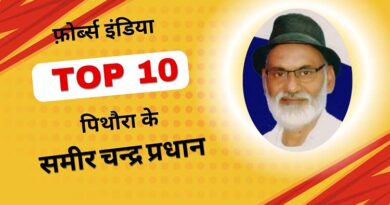सिंधु घाटी से आधुनिक भारत तक शक्ति पूजा की अखंड परंपरा

भारतीय सभ्यता का इतिहास केवल राजवंशों, युद्धों और साम्राज्यों का इतिहास नहीं है, बल्कि यह मान्यताओं, आस्थाओं और धार्मिक परंपराओं का भी जीवंत आख्यान है। इन्हीं परंपराओं में शक्ति की उपासना का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति में शक्ति को सृष्टि और अस्तित्व की मूल ऊर्जा माना गया है। यह विश्वास रहा है कि बिना शक्ति के शिव भी शून्य हैं और शक्ति ही वह तत्व है जो जगत की गति और जीवन की धारा को संचालित करता है। यही कारण है कि भारत में शाक्त धर्म का विकास हड़प्पा सभ्यता से लेकर आधुनिक समय तक निरंतर होता रहा और समय-समय पर राजाओं और प्रजा, दोनों ने इसे अपनी आस्था का केंद्र बनाया।
हड़प्पा सभ्यता और मातृदेवी की पूजा
यदि हम प्रारंभिक इतिहास की ओर देखें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाइयों में मातृदेवी की मूर्तियाँ और मिट्टी से बनी प्रतिमाएँ मिली हैं। इन प्रतिमाओं में देवी को प्रजनन और उर्वरता का प्रतीक माना गया है। धरती माता का यह स्वरूप कृषि आधारित समाज की मूलभूत आवश्यकता, अन्न और जीवन की निरंतरता से जुड़ा था। उस समय स्त्री को जीवनदायिनी शक्ति के रूप में सम्मान दिया जाता था। यह परंपरा शाक्त धर्म की प्रारंभिक जड़ों का परिचायक है।
वैदिक और उत्तरवैदिक युग में देवियों का स्वरूप
वैदिक काल में देवताओं का स्वरूप अपेक्षाकृत पुरुषप्रधान रहा। इंद्र, अग्नि, वरुण जैसे देवताओं का उल्लेख अधिक मिलता है, किंतु देवियों की उपस्थिति भी स्पष्ट है। ऋग्वेद में उषा को भोर की देवी, अदिति को अनंत आकाश की जननी और सरस्वती को ज्ञान की अधिष्ठात्री के रूप में वर्णित किया गया है। यद्यपि इन देवियों को सर्वोच्च सत्ता का स्थान नहीं मिला, परंतु यह संकेत अवश्य मिलता है कि शक्ति की अवधारणा भारतीय चिंतन में गहराई से निहित थी।
उत्तरवैदिक युग में यह विचार और परिपक्व हुआ। देवियों को केवल सहायक शक्ति न मानकर स्वतंत्र सत्ता के रूप में देखने की परंपरा विकसित हुई। यही वह बिंदु है जहाँ से शाक्त धर्म का संगठित स्वरूप बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है।
पुराणकाल और शक्ति की सर्वोच्चता
महाभारत और पुराणों के युग में शक्ति की उपासना ने संगठित रूप धारण कर लिया। मार्कण्डेय पुराण का दुर्गा सप्तशती इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। इसमें देवी को महिषासुरमर्दिनी, चामुंडा, कात्यायनी और चंडिका जैसे विविध रूपों में वर्णित किया गया है। यहाँ देवी को केवल पूजनीय नहीं, बल्कि सृष्टि, पालन और संहार की स्वतंत्र शक्ति माना गया।
देवी महात्म्य में एक विशेष बात यह कही गई है कि देवता स्वयं असहाय होकर शक्ति से प्रार्थना करते हैं और वही उन्हें बल प्रदान करती है। यह विचार भारतीय धार्मिक परंपरा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन था, क्योंकि यहाँ देवी को ब्रह्म के समान सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित किया गया।
गुप्तकाल और शाक्त साधना का विस्तार
गुप्त साम्राज्य के समय (चौथी–छठी शताब्दी ई.) शाक्त धर्म को राजकीय संरक्षण मिला। गुप्त राजाओं ने शक्ति मंदिरों का निर्माण करवाया और कला में देवी की मूर्तियों का भव्य स्वरूप सामने आया। इस काल में तांत्रिक साधना का भी प्रसार हुआ। देवी को केवल धार्मिक आस्था का केंद्र न मानकर ध्यान, साधना और योग का आधार भी माना गया।
देवी को ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा के रूप में देखने की प्रवृत्ति दार्शनिक स्तर पर भी स्पष्ट हुई। “शक्ति ही शिव का प्राण है” इस धारणा ने भारतीय आध्यात्मिक चिंतन में गहरा स्थान बना लिया।
मध्यकालीन भारत और राजाओं की शक्ति उपासना
मध्यकाल में शाक्त धर्म ने और व्यापक स्वरूप ग्रहण किया। बंगाल, ओडिशा, असम और छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों में तंत्र और शाक्त परंपराएँ गहराई से जड़ें जमाती चली गईं। पाल और सेन राजाओं ने बंगाल में शक्ति की उपासना को राजकीय संरक्षण दिया। देवी तारा, काली और चामुंडा की पूजा इस क्षेत्र में विशेष रूप से प्रतिष्ठित हुई।
दक्षिण भारत में चोल राजाओं ने दुर्गा और काली की मूर्तियों का मंदिरों में भव्य रूप से प्रतिष्ठान किया। कर्नाटक और तमिलनाडु में देवी को “अम्मन” और “अम्मा” के रूप में पूजने की परंपरा आज तक जारी है।
मध्य भारत में चंदेलों, कलचुरियों और नागवंशियों ने भी शक्ति पूजा को बढ़ावा दिया। खजुराहो के मंदिरों में देवी की मूर्तियाँ आज भी शाक्त परंपरा की समृद्धि का प्रमाण हैं।
राजस्थान के राजाओं की शक्ति पूजा
राजस्थान में शक्ति पूजा का महत्व विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यहाँ के शासक शक्ति को अपनी कुलदेवी और विजय की अधिष्ठात्री मानते थे।
-
मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी अरावली पर्वत स्थित बनास नदी तट पर स्थित बाणेश्वरी माता तथा अम्बा माता मानी जाती थीं। महाराणा प्रताप युद्ध पर जाने से पूर्व देवी की पूजा अवश्य करते थे।
-
मारवाड़ (जोधपुर) के राठौड़ शासकों की कुलदेवी नागौर की नागणेची माता थीं। वे युद्ध से पहले नागणेची माता के मंदिर में जाकर आशीर्वाद लेते थे।
-
जैसलमेर के भाटी राजपूत तनोट माता और लाठियाल माता को पूजते थे। आज भी तनोट माता का मंदिर भारत–पाक सीमा पर भारतीय सैनिकों की आस्था का केंद्र है।
-
बूंदी और कोटा के हाड़ा राजपूतों की कुलदेवी करणी माता तथा चामुंडा माता थीं।
-
जयपुर के कछवाहा राजाओं ने शक्ति की पूजा के लिए अम्बा माता का भव्य मंदिर बनवाया, जो आज “अमेर का अंबाजी मंदिर” कहलाता है।
राजस्थान के राजाओं ने शक्ति की पूजा को केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं रखा। उनके लिए यह राजनीति और युद्ध नीति का भी एक आवश्यक अंग था। युद्ध से पहले विजय का आशीर्वाद लेने, नए किलों की नींव रखने और राजतिलक के समय देवी का आह्वान करना अनिवार्य परंपरा थी।
प्रजा भी इन कुलदेवियों को अपनी रक्षक मानती थी। यही कारण है कि राजस्थान में शक्ति पूजा जन-जन की आस्था बन गई और यह परंपरा आज भी नवरात्र और अन्य पर्वों पर बड़े उत्साह से जीवित है।
छत्तीसगढ़, ओडिशा और बस्तर में लोकशक्ति की पूजा
भारत के मध्य और पूर्वी अंचलों में शक्ति पूजा का लोक रूप अधिक दिखाई देता है। छत्तीसगढ़ और बस्तर में ग्रामदेवियों की पूजा व्यापक है। यहाँ की जनता ने जंगल, पहाड़ और नदियों को शक्ति का स्वरूप मानकर पूजा की। मावली माता, दंतेश्वरी माता जैसे स्वरूप ग्रामीण और जनजातीय समाज में देवी के प्रति गहरे विश्वास को प्रकट करते हैं।
कलचुरी और नागवंशी शासकों ने इन लोकदेवियों को राजकीय संरक्षण दिया। दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माता का मंदिर आज भी जनजातीय समाज और पूरे छत्तीसगढ़ की शक्ति आराधना का प्रमुख केंद्र है।
आधुनिक काल और शक्ति पूजा की निरंतरता
आज भी भारत में शक्ति पूजा उतनी ही सजीव है। नवरात्र, दुर्गा पूजा, दशहरा, शक्ति पीठ यात्राएँ और सार्वजनिक उत्सव इस आस्था को निरंतर प्रकट करते हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में महिलाएँ देवी को शक्ति स्वरूपा मानकर आत्मबल और प्रेरणा प्राप्त करती हैं।
सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी शक्ति पूजा का प्रभाव दिखाई देता है। चुनावी सभाओं से लेकर जन-आंदोलनों तक देवी के जयघोष सुनाई देते हैं। धार्मिक पर्यटन और शक्ति पीठ यात्राओं ने आधुनिक समाज में भी शक्ति की उपासना को महत्त्वपूर्ण बना दिया है।
इस प्रकार स्पष्ट है कि शाक्त धर्म का विकासक्रम भारतीय इतिहास की निरंतर धारा है। हड़प्पा की मातृदेवी से लेकर वेदों की देवियाँ, पुराणों की महिषासुरमर्दिनी, गुप्तकालीन तांत्रिक साधना, मध्यकालीन राजाओं की कुलदेवियाँ और आधुनिक काल के नवरात्र पर्व,ये सभी चरण दर्शाते हैं कि शक्ति पूजा केवल धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि सांस्कृतिक जीवन का आधार रही है।
राजस्थान के राजाओं से लेकर छत्तीसगढ़ के ग्राम्य समाज तक, शक्ति को रक्षक, पोषक और विजयदात्री के रूप में पूजा गया। प्रजा और शासक, दोनों ने संकट की घड़ी में देवी की शरण ली और उसे अपने जीवन का मार्गदर्शक माना।
आज भी जब भारत में करोड़ों लोग शक्ति की आराधना करते हैं, तो यह परंपरा हमें याद दिलाती है कि शक्ति केवल देवी का रूप नहीं, बल्कि मनुष्य की आंतरिक ऊर्जा और संघर्षशीलता का भी प्रतीक है। यही शाक्त धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है, जिसने इसे युगों-युगों तक जीवंत बनाए रखा है।