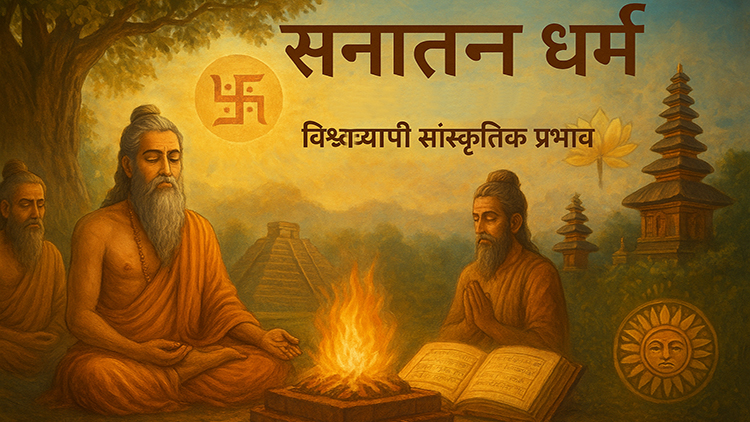सनातन धर्म के शाश्वत सिद्धांत और विश्वव्यापी सांस्कृतिक प्रभाव

सनातन का अर्थ है शाश्वत। नियमों या अतीत, सिद्धांतों का वह समूह जो वर्तमान और भविष्य के सभी समयों के लिए सत्य है तथा संसार के सभी प्राणियों, जीवों और मनुष्यों के मानवता को इस जीवन और परलोक में सदैव सही मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन प्रदान करता है, सनातन धर्म कहलाता है। चूँकि इसके सिद्धांतों का सबसे प्राचीन अभिलेख वेदों में मिलता है, इस धर्म को वैदिक धर्म भी कहा जाता है,
किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को – न तो किसी अवतार को, न ही किसी मंत्रद्रष्टा या ऋषि को – इस धर्म के प्रवर्तक के रूप में पहचाना जा सकता है। इसीलिए यह एक धर्म से कहीं बढ़कर है। यहाँ तक कि वेदों को भी अपौरुषेय (मानव उत्पत्ति नहीं) माना जाता है क्योंकि उनके मंत्र ऋषियों द्वारा देखे गए थे, उनके द्वारा रचे नहीं गए थे।
इस धर्म के नियम और सिद्धांत सार्वभौमिक ब्रह्मांडीय सत्य हैं जो सदा विद्यमान रहते हैं। सनातन शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में किया गया है; वास्तव में, इस धर्म को मूलतः केवल धर्म कहा जाता था। प्राचीन काल में यह एकमात्र प्रचलित धर्म था, इसलिए इसका कोई विशिष्ट नाम नहीं था। ‘हिंदू’ शब्द, जो प्रचलित है, इस धर्म के किसी भी प्राचीन ग्रंथ में नहीं मिलता। यह शब्द भारत में बाद में अरबी और फारसी संपर्कों के साथ, और इस्लामी आक्रमणों के साथ और भी अधिक प्रबलता से आया। ऐसा कहा जाता है कि इन पश्चिम एशियाई देशों के लोग सिंधु नदी का नाम हिंदू और उसके निकटवर्ती भूभाग का नाम हिंद उच्चारित करते थे। वे इस भूमि के निवासियों को हिंदू कहते थे और समय के साथ, यह शब्द इस भूमि के धर्म से भी जुड़ गया।
आरंभ में, केवल एक ही धर्म था और आस्था की कोई अन्य व्यवस्था नहीं थी। उस समय विश्व के विभिन्न भागों में जो भी धार्मिक क्रियाएँ या अनुष्ठान प्रचलित थे, वे सभी एक ही सार्वभौमिक धर्म पर आधारित थे। धर्म और संस्कृति काफ़ी हद तक एक-दूसरे के पूरक थे। सनातन धर्म पर आधारित संस्कृति के पुरातात्विक साक्ष्य विश्व के सभी भागों में पाए जाते हैं।
एशिया माइनर (तुर्की) में हुए उत्खनन से दो राजाओं, मितानी के रामेसेस द्वितीय और हित्ती राजा, के बीच हुई एक संधि के शिलालेख मिले हैं। यह संधि 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी और इसमें प्रसिद्ध वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र और वरुण के नाम अंकित हैं, जो इस संधि के साक्षी थे। यह इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि उस समय और उससे भी पहले उस क्षेत्र में वैदिक धर्म का प्रचलन था।
अमेरिकी महाद्वीप के मेक्सिको में, राम-सीता नाम से एक पुराना पारंपरिक उत्सव आज भी नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है, जब भारत में रामलीला होती है। राम और सीता भारतीय महाकाव्य रामायण के नायक और नायिका के नाम हैं, और दोनों को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के अवतार के रूप में जाना जाता है।
राम का जन्म सूर्यवंश (सूर्य कुल) में हुआ था। मेक्सिको में हुए उत्खननों से न केवल प्राचीन मेक्सिकोवासियों, जिन्हें माया कहा जाता है, के अत्यंत विकसित स्थापत्य और मूर्तिकला कौशल का पता चला है, बल्कि उनके धार्मिक रीति-रिवाजों का भी पता चला है। वे सूर्य देव की पूजा करते थे और उनके पास सूर्य, जो एक वैदिक देवता हैं, के मंदिर थे। इनमें स्वस्तिक और कमल पुष्प की नक्काशी पाई जाती है। मंदिर स्पष्ट रूप से माया धर्म और संस्कृति के भारतीय संबंध का संकेत देते हैं। महाभारत में माया का उल्लेख इंद्रप्रस्थ (दिल्ली) स्थित पांडवों के महल के शिल्पकार-वास्तुकार के रूप में मिलता है। आज भी, चटाई पर बैठकर भारतीय भोजन करने वाले मैक्सिकन लोगों का रहन-सहन, खान-पान और स्वभाव भारतीयों से मिलता-जुलता है।
दक्षिण अमेरिका के पेरू और बोलीविया के लोग, मेक्सिकोवासियों के साथ, मानते हैं कि उनकी संस्कृति भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई है। उनके पूर्वज इंका कहलाते थे और वे सूर्य देव की पूजा करते थे। संस्कृत में इना का अर्थ सूर्य होता है। होंडुरास में, सनातन धर्म के त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश – और गणेश, शेषनाग, नृसिंह आदि की मूर्तियाँ खुदाई में मिली हैं।
दक्षिण पूर्व एशिया के अधिकांश हिस्सों में, हालांकि आज प्रचलित धर्म या तो बौद्ध धर्म है जो सनातन धर्म की एक शाखा है – या इस्लाम, भारतीय संस्कृति अभी भी न केवल मंदिरों और अन्य भौतिक अवशेषों जैसे स्मारकों के रूप में, बल्कि राम-लीला जैसे सामाजिक लोकाचार और परंपराओं और महाभारत और पुराणों की कहानियों के रूप में भी मौजूद है।
इंडोनेशिया का बाली द्वीप धार्मिक रूप से भी हिंदू के रूप में जाना जाता है। हालांकि, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के साथ दक्षिण पूर्व एशियाई संबंध अपेक्षाकृत बाद में शुरू हुआ; पहली शताब्दी ईस्वी और 15वीं शताब्दी ईस्वी के बीच भारतीय मूल के कई राजाओं और राजवंशों ने वहां शासन किया। कंबु, कौंडिन्य, शैलेंद्र, राजेंद्र कोला आदि जैसे अग्रदूतों ने न केवल अपने साम्राज्य स्थापित किए बल्कि धर्म और संस्कृति के चक्र को भी गति दी।
कभी-कभी विश्व धर्मों की प्रसिद्ध कथाओं पर चिंतन रोचक होने के साथ-साथ ज्ञानवर्धक भी सिद्ध होता है। उदाहरण के लिए, बाइबिल के ओल्ड टेस्टामेंट की एक कथा की तुलना उपनिषदीय रूपक से करने पर वह आँखें खोलने वाली हो जाती है। उपनिषदों (मुंडक और श्वेतावतार) में एक रूपक मिलता है: दो पक्षी पीपल के वृक्ष पर बैठे हैं। उनमें से एक वृक्ष का फल खाता है, जबकि दूसरा केवल देखता रहता है। यहाँ जो पक्षी पीपल का फल (इंद्रिय भोग) खाता है, उसे जीव कहते हैं, और जो नहीं खाता, वह ब्रह्म है।
सेमेटिक धर्मों में एक कथा प्रचलित है जिसमें दम्पति आदम और हव्वा को अदन के बगीचे में सेब के वृक्ष का फल खाने से मना किया गया था। आदम ने नहीं खाया, परन्तु हव्वा ने वह फल खा लिया। बाद में, आदम ने भी वह फल खाया। इस कथा में, उपनिषदीय वृक्ष और पीपल का फल निषिद्ध फल बन जाते हैं। जीव हव्वा बन जाता है और आत्मा आदम बन जाती है, जो, कहानी के अनुसार, शुरुआती अनिच्छा के बाद अंततः फल खा लेता है। यह उपनिषदीय रूपक का ही एक और रूप है, हालाँकि विकृत।
ये अनेक उदाहरणों में से कुछ उदाहरण मात्र हैं जो दर्शाते हैं कि मूलतः सम्पूर्ण विश्व में केवल एक ही धर्म था, जो न केवल सनातन था, बल्कि सर्वव्यापी भी था। इसमें धार्मिकता पर बल दिया गया था, न कि किसी सांप्रदायिक धर्म पर, न कि केवल धर्म पर। इसके बारे में एक उल्लेखनीय तथ्य यह रहा है कि इसे पूरे विश्व में स्वेच्छा से स्वीकार किया गया। इसे कभी भी किसी अनिच्छुक व्यक्ति पर बलपूर्वक नहीं थोपा गया, न ही धर्मांतरण के तरीकों से इसका प्रचार किया गया। इसे इसलिए स्वीकार किया गया क्योंकि यह उच्च मूल्यों का एक समूह था।
‘सनातन धर्म’ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मनुस्मृति और महाकाव्य महाभारत में हुआ है, जहाँ हमें सनातन धर्म के रूप में पहचाने जाने वाले कुछ उत्तम गुणों या जीवन के उच्च मूल्यों का वर्णन मिलता है। मनु कहते हैं: “सत्य बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, परन्तु न तो कटु सत्य बोलना चाहिए और न ही मीठा झूठ। यही सनातन धर्म है” (एषा धर्म सनातनः मनुस्मृति 4/138)। महाभारत में भी सत्य को सनातन धर्म बताया गया है (शांति पर्व 164/4)। इसमें सभी प्राणियों के प्रति अद्रोह, दया और उपकार करने, तथा दान देने को भी सनातन धर्म बताया गया है (शांति पर्व 162/2)। महाकाव्य में वर्णाश्रम धर्म सहित अन्य नैतिक मानदंडों और गुणों का भी सनातन धर्म के रूप में वर्णन किया गया है। विशिष्ट विशेषताएँ
विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों, प्रणालियों या विद्यालयों के विकास के साथ, सनातन धर्म के अंतर्गत कई धार्मिक संप्रदाय विकसित हुए, लेकिन कुछ विशिष्ट विशेषताएं अभी भी समान हैं, ये सभी के लिए, या कम से कम मुख्यधारा द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। ये हैं:
कर्म सिद्धांत:
भौतिकी के इस सिद्धांत की तरह कि प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, सनातन धर्म ने कर्म और कर्मफल का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जिसके अनुसार मनुष्य के प्रत्येक अच्छे या बुरे कर्म का, समय आने पर एक परिणाम अवश्य भोगना पड़ता है – अच्छे कर्म का सुखद फल (परिणाम) और बुरे कर्म का कड़वा फल। वर्तमान जन्म में हमारे लाभ और हानि, काफी हद तक हमारे पूर्वजन्मों के, शायद पूर्वजन्मों के, पुण्य या पाप कर्मों का परिणाम हैं, और हमारे वर्तमान कर्मों का फल हमें भविष्य में, शायद अगले जन्मों में, भोगना पड़ेगा, क्योंकि सभी कर्मों का फल इसी जन्म में भोगना नहीं पड़ता।
पुनर्जन्म:
कर्म के सिद्धांत से निकटता से जुड़ा है पुनर्जन्म का सिद्धांत। हम जानते हैं कि सभी प्राणी और यहाँ तक कि सभी मनुष्य भी समान रूप से भाग्यशाली नहीं होते। यदि जीवन में केवल एक ही जन्म होता, तो एक अबोध शिशु जो बीमार होकर जन्म से ही मर जाता है, या जो जीवित तो रहता है, लेकिन जन्म से ही लंगड़ा या अंधा होता है, उससे क्या पाप होता है? कोई सुंदर क्यों होता है, कोई कुरूप? कोई बुद्धिमान क्यों होता है और कोई मंद क्यों? यदि ईश्वर पक्षपाती और दयालु नहीं है, तो मनुष्यों में इन अंतरों को कर्मफल और पुनर्जन्म के सिद्धांतों के बिना समझाया नहीं जा सकता। ईश्वर हमें एक या एक से अधिक जन्मों में अपने आचरण सुधारने के अवसर प्रदान करता है। परा-मनोवैज्ञानिक प्रमाण इसका समर्थन करते हैं।
जीवन के चार लक्ष्य (पुरुषार्थ चतुष्टय):
सनातन धर्म ने मानव जीवन के चार उद्देश्य प्रतिपादित किए हैं: धर्म (धार्मिकता), अर्थ (धन और पद), काम (भोग), और मोक्ष (मुक्ति)। धर्म, धार्मिकता, समाज या मानवता के सर्वांगीण विकास और पोषण के अनुरूप है। अर्थ में भौतिक कल्याण शामिल है। काम, संयमित रूप से जीवन का वैध आनंद है। और इन सबसे बढ़कर, जीवन का अंतिम या परम लक्ष्य, मोक्ष है, जिसका अर्थ है बार-बार जन्म-मृत्यु के सांसारिक बंधनों से मुक्ति और आनंद (स्वयं की शाश्वत आनंदमय अवस्था) की प्राप्ति।
वर्णाश्रम धर्म:
समाज चार व्यावसायिक वर्गों में विभाजित है, जिन्हें वर्ण कहा जाता है, अर्थात, ब्राह्मण (विद्वान, तपस्वी, धर्मपरायण पुरुषों का पुजारी और शिक्षक वर्ग), क्षत्रिय (राष्ट्र और समाज में कमजोर लोगों की रक्षा के लिए योद्धा वर्ग), वैश्य (उत्पादन और वितरण के लिए कृषक, पशुपालक और व्यापारी वर्ग), और शूद्र (अपने कर्तव्यों को पूरा करने में अन्य सभी की सहायता करने वाला सेवा वर्ग)। इसी प्रकार, मानव के व्यवस्थित विकास और जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनकी सहायता के लिए, जीवन की पूरी अवधि को चार आश्रमों (अवस्थाओं) में विभाजित किया गया है, अर्थात्, ब्रह्मचर्यश्रम (25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचारी विद्यार्थी जीवन), गृहस्थ (विवाह के बाद गृहस्थ, अपने परिवार और अन्य अवस्थाओं के सदस्यों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी संभालना), वानप्रस्थ (गृहस्थ अवस्था से निवृत्त होने के बाद तपस्या और सामाजिक कल्याण का एक साधु जीवन व्यतीत करना), और संन्यास (सभी सांसारिक औपचारिकताओं का त्याग और आत्म-मुक्ति के एकसूत्रीय कार्यक्रम का अनुसरण करना, दूसरों को भी ऐसी मुक्ति प्राप्त करने में सहायता करना)।
भगवान का अवतार:
सनातन धर्म में यह भी कहा गया है कि जब भी पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं और धर्म की पुनः स्थापना करते हैं।