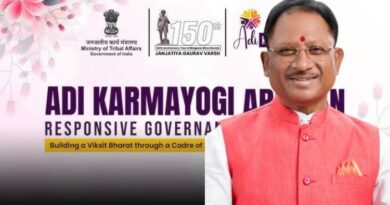नागपंचमी से नागवंश तक संस्कृति में छिपा है जैव विविधता संरक्षण का मंत्र

भारतीय प्राचीन संस्कृति में प्रकृति के प्रत्येक कण को देवतुल्य स्थान प्राप्त है। इसमें चाहे वृक्ष हों, नदियाँ, पर्वत, पशु-पक्षी या फिर सर्प हों। सबके प्रति हमारे पुरखों ने आदर और कृतज्ञता का भाव बनाए रखा है। इसीलिए नागों की पूजा, उनके प्रति भय के बजाय श्रद्धा, और उनके संरक्षण की परंपरा हमारे पुरखों की वैज्ञानिक सोच एवं प्रकृति के प्रत्येक जीवन को अपना कुटुम्बी मानने की परम्परा का परिचायक है। धार्मिकता से रची बसी यह परम्परा परोक्ष रुप से जैवविविधता के संरक्षण की एक चुपचाप चलने वाली सतत धार्मिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है जो एक पीढी से दुसरी पीढी को विरासत के रुप में हस्तांतरित होती है।
भारतीय किसान परम्परा से जानते हैं कि नाग कृषि व्यवस्था के मित्र हैं। खेतों में चूहों, मेंढकों और कीटों को भोजन बनाकर उनकी संख्या नियंत्रित कर फसलों की रक्षा करते हैं। यह प्रकृति प्रदत्त उपहार स्वरुप जैव-नियंत्रण प्रणाली का उदाहरण है। नागों के बिना यह संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे चूहों और अन्य हानिकारक जीवों की आबादी बढ़कर खेती को नुकसान पहुँचा सकती है।
छत्तीसगढ़ में नागों के प्रति विशेष श्रद्धा दिखाई देती है। वहाँ नागपंचमी के दिन किसान अपने खेतों में नाग-नागिन की पूजा कर दूध और लाई अर्पित करते हैं। यह परंपरा केवल धार्मिक भाव नहीं, बल्कि मानव और जीव-जंतु के बीच सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व की भावना का प्रतीक है।
नागों को भारतीय लोकमानस में गुप्त वैभव, रहस्यमयी ऊर्जा और अदृश्य शक्ति का प्रतीक माना गया है। नाग जिस तरह जमीन के नीचे बिलों में रहते हैं, वे भूमिगत पारिस्थितिक तंत्र के अहम भाग हैं। बांबियाँ, झाड़ियाँ, चट्टानों की दरारें आदि उनके रहने की जगहें अक्सर उन जैविक आवासों का हिस्सा होती हैं जहाँ अनेक छोटे जीव-जन्तु रहते हैं। नागों का अस्तित्व इन सूक्ष्म पारिस्थितिकी प्रणालियों को स्थिर रखने में सहायक होता है।
नागों की उपस्थिति उस पारिस्थितिक संतुलन का भी प्रतीक है, जिसमें हर जीव की अपनी भूमिका है। यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र से नाग जैसे शिकारी जीव लुप्त हो जाएँ, तो खाद्य श्रृंखला टूट जाएगी और जैव विविधता असंतुलित हो जाएगी।
भारतीय शास्त्रों में नागों का उल्लेख अनेक रूपों में मिलता है, शेषनाग के रूप में पृथ्वी को धारण करने वाले, शिव के गले में वासुकि के रूप में काल के बोधक, विष्णु की शैय्या के रूप में अनंत। ये रूपक मात्र धार्मिक प्रतीक नहीं हैं, बल्कि उस चेतना के द्योतक हैं जिसमें जीवों के अस्तित्व को धर्म से जोड़कर उसे संरक्षण योग्य पुज्य बनाया गया।
नागपंचमी जैसे पर्वों का महत्व इसी संदर्भ में और बढ़ जाता है। यह पर्व वर्षा ऋतु के मध्य में आता है, जब सांपों का अपने बिलों से बाहर निकलना आम बात होती है। इस समय उन्हें भोजन की तलाश होती है, और वे अक्सर मानवीय बस्तियों के पास भी आ जाते हैं। ऐसे समय में नागपंचमी की पूजा और पूजन की परंपराएं लोगों को यह सिखाती हैं कि नागों को मारा न जाए, बल्कि उन्हें सम्मानपूर्वक सुरक्षित स्थानों तक जाने दिया जाए। यह लोकपरंपरा जैवविविधता को समझकर संरक्षण करने की उद्दात विरासत है।
छत्तीसगढ़ अंचल की ‘नगमत’ परंपरा, जिसमें गुरु शिष्य को ‘सपहर मंत्र’ प्रदान करता है, भी नागों के साथ सहजीवन की मिसाल है। इस परंपरा में सर्प के प्रति आदर, उसकी शक्ति का आह्वान और उसका सम्मान सब कुछ समाहित है। यह जैवविविधता संरक्षण का मौन लेकिन सशक्त लोकपाठ है, जहाँ सर्पों के साथ ज्ञान, मंत्र, औषधि और अनुशासन जुड़ा हुआ है। नगमत के समापन पर दी जाने वाली कड़वी औषधि यह संदेश देती है कि विष से भी रक्षा संभव है, बशर्ते हम प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलें।
भारत के प्राचीन मंदिरों के स्थापत्य में नागों का जो अंकन मिलता है, वह केवल शिल्प नहीं, एक भावनात्मक और सांस्कृतिक चेतना का दिखाई देने वाला रूप है। मुख्य द्वारों पर नागवल्लरी, शेष शैय्या पर विष्णु, शिव के गले में वासुकि, मूर्तियों में नागकन्याएं आदि का शिल्पांकन हमें बार-बार नागों के महत्व और उनके संरक्षण की याद दिलाते हैं।