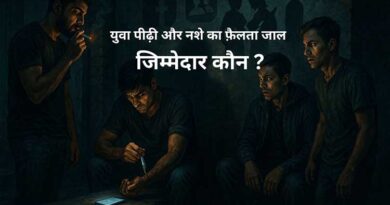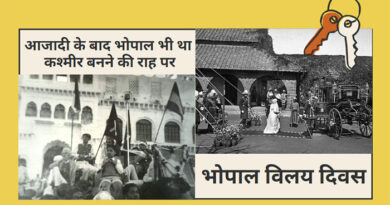मानव सभ्यता की मार्गदर्शक और ज्ञान का प्राचीन स्रोत पुस्तकें

कोई अभागा ही होगा जिसने कभी कोई पुस्तक अपने हाथों में न ली होगी और हाथों में ली होगी तो पढी न होगी, पढी होगी तो उसके मानस में विचारों ने जन्म न लिया होगा। बस इन्हीं विचारों से मनुष्य का जीवन प्रकाश से भर जाता है जो आजीवन आलोकित रहता है। पुस्तकें मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं जिन्हें हम वर्तमान में पुस्तकें, किताब कहते हैं उन्हें प्राचीन काल में ग्रंथ कहा जाता था, ये ग्रंथ ज्ञान के प्राचीनतम स्रोत हैं, जो आज भी मानव सभ्यता का मार्गदर्शन कर रहे हैं।
ये ग्रंथ मानव सभ्यता की बौद्धिक और सांस्कृतिक यात्रा की अमूल्य धरोहर हैं। जब मनुष्य ने अपनी भावनाओं, विचारों और ज्ञान को संरक्षित करने की आवश्यकता महसूस की, तब श्रुति से स्मृति के रुप में लेखन कला का विकास हुआ। प्रारंभ में यह कार्य पत्थरों, ताड़-पत्रों, भोजपत्रों या मिट्टी की पट्टियों पर किया जाता था। धीरे-धीरे जैसे-जैसे लेखन शैली और सामग्री का विकास हुआ, वैसे ही ग्रंथ के रुप में वर्तमान पुस्तक का प्रारूप भी विकसित हुआ।
विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद को माना जाता है, जो वैदिक संस्कृत में रचित है और लगभग 1500 ईसा पूर्व से भी पहले का ग्रंथ है। ऋग्वेद न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत है, बल्कि उसमें उस काल की सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण की झलक भी मिलती है। भारतवर्ष में ज्ञान की परंपरा, प्राचीनता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण वेद है।
महर्षि दयानंद ने वेदों का ज्ञान का सागर कहा है। उन्होंने आहवान किया कि “वेदों की और लौटो।“ चारों वेदों में पृथक पृथक विषय हैं। देवताओं की स्तुतियों का संग्रह ऋग्वेद है, यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधियों का विवरण है, कर्मकांड का वेद है। सामवेद में ऋचाओं का गायन स्तुति रूप है जो संगीत से संबंधित हैं तथा अथर्ववेद जीवन संचालन कि विद्या सिखाता है जिसका विषय औषधि, घरेलू जीवन आदि पर आधारित है।
उपनिषद दार्शनिक ग्रंथ है, जो ब्रह्म और आत्मा के रहस्य को समझाते हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण आदर्श जीवन, धर्म, कर्तव्य और आदर्श शासक राम की गाथा है। ऋषि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है जिसमें जीवन के प्रत्येक पक्ष का वर्णन है। भगवद्गीता इसी का भाग है।
भारत का प्राचीन साहित्य अत्यंत व्यापक, विविध विषयक एवं ज्ञान से भरा हुआ है। इस मार्गदर्शक साहित्य को वेद, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, स्मृतियाँ, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, ज्योतिष और साहित्य में बाँटा जा सकता है। ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर ॠषियों ने अपनी दृष्टि नहीं डाली हो। मानव के जीवन को अनुशासनबद्ध करने के लिए उन्होंन लोक कल्याण की दृष्टि से ग्रंथो की रचना की तथा आज भी पुस्तकों के रुप में ग्रंथ रचे जा रहे हैं क्योंकि जीवन को दिशा देने में पुस्तकों का महत्वपूर्ण योगदान है। ये हमें सोचने, समझने और बुद्धि का उपयोग कर निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती हैं तथा शिक्षा, नैतिकता, विज्ञान, कला, इतिहास और साहित्य आदि जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करती हैं।
प्राचीन काल से ही पुस्तकें शिक्षा प्रणाली की रीढ़ रही हैं। विद्यार्थियों में बौद्धिक क्षमता का विकास पुस्तकों से ही संभव होता है। अच्छे विचारों से भरी पुस्तकें मनुष्य के चरित्र निर्माण में सहायता करती हैं। रामायण, महाभारत, गीता जैसे ग्रंथ आज भी नैतिक मूल्यों का संचार करते हैं। साहित्य, कविता, उपन्यास, कहानियाँ आदि रचनात्मकता को जन्म देती हैं तथा मानव मस्तिष्क की कल्पना शक्ति को भी उड़ान देती हैं।
भारत की प्राचीन पुस्तकों और ग्रंथों ने यह सिद्ध किया है कि ज्ञान की परंपरा यहाँ सहस्राब्दियों से जीवित है। वेदों से लेकर नाट्यशास्त्र और आयुर्वेद तक, हर ग्रंथ मनुष्य के जीवन को उन्नत बनाने में सहायक रहा है। आज की पुस्तकें उसी ज्ञान-संस्कृति की विरासत हैं। इसलिए कहा गया है –
“नास्ति विद्या समं चक्षुः, नास्ति सत्य समं तपः।”
(विद्या से बढ़कर कोई दृष्टि नहीं, और सत्य से बड़ा कोई तप नहीं।)